10 दिसंबर को भारत और दक्षिण कोरिया ने अपने उतार-चढ़ाव भरे द्विपक्षीय संबंधों (1973-2023) के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया।
 |
| दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक येओल और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर 2023 में नई दिल्ली में ग्रुप ऑफ 20 (जी20) शिखर सम्मेलन के दौरान। (स्रोत: एएनआई) |
इस अवसर पर एक बयान में, दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सूक येओल ने भारत के साथ विशेष रणनीतिक साझेदारी को मज़बूत करने की आशा व्यक्त की। सोशल नेटवर्क एक्स पर लिखते हुए, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्टि की: भारत-दक्षिण कोरिया संबंध "आपसी सम्मान, साझा मूल्यों और बढ़ती साझेदारी की यात्रा" हैं।
“ठंडे” से “गर्म” तक
कोरियाई युद्ध को रोकने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, शीत युद्ध ने दक्षिण कोरिया के साथ भारत के संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया। शुरुआत में, 1973 में दक्षिण कोरिया के साथ संबंध स्थापित करने की भारत की पहल को महज एक कूटनीतिक कदम माना गया, जिससे कोई खास प्रगति की उम्मीद नहीं थी।
लेकिन शीत युद्ध की समाप्ति एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। पूर्वी एशियाई देशों की तेज़ आर्थिक वृद्धि से प्रभावित होकर, एशियाई नेताओं, खासकर भारत के नेताओं ने दक्षिण कोरिया और जापान की सफलता में गहरी दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। उसी समय, जब सियोल अपनी निर्यात-आधारित अर्थव्यवस्था के लिए नए बाज़ार तलाश रहा था, उसके राजनीतिक और व्यावसायिक नेता तेज़ी से भारत की ओर मुड़ रहे थे।
साझा हितों से प्रेरित होकर भारत और दक्षिण कोरिया ने समझौतों का एक नया नेटवर्क बनाया है, जिससे दोनों देशों को अपने संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
फरवरी 1996 में दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति किम यंग सैम की नई दिल्ली यात्रा एक मील का पत्थर थी, जिसमें उन्होंने भविष्योन्मुख साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए, तथा 2000 तक द्विपक्षीय व्यापार को 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा। इसके बाद, दोनों देशों के नेताओं ने कोरिया-भारत संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना था।
2004 में, दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति रोह मू ह्यून की भारत यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने शांति और समृद्धि के लिए दीर्घकालिक सहकारी साझेदारी की स्थापना की, जिसका लक्ष्य 2008 तक व्यापार कारोबार को 10 बिलियन अमरीकी डॉलर तक बढ़ाना था। एक वर्ष बाद, दोनों पक्षों ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) पर हस्ताक्षर किए, जो जनवरी 2010 से प्रभावी हुआ।
उल्लेखनीय है कि तेज़ी से बदलती दुनिया में साझेदारी के विकास के साथ, भारत और दक्षिण कोरिया दोनों ही रणनीतिक रूप से अधिक सक्रिय होते जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए, 2010 में, नई दिल्ली और सियोल ने एक रणनीतिक साझेदारी स्थापित की, जिसमें सीमा सुरक्षा और रक्षा सहयोग शामिल है।
पाँच साल बाद, दोनों देशों ने अपने संबंधों को एक विशेष रणनीतिक साझेदारी तक उन्नत किया और द्विपक्षीय यात्राओं और बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से वार्षिक उच्च-स्तरीय बैठकों की रूपरेखा तैयार की। सियोल और नई दिल्ली ने विदेश मामलों और रक्षा पर 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता शुरू की।
दोनों नेताओं की पिछली मुलाकात सितंबर 2023 में नई दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। इस दौरान, राष्ट्रपति यून सुक येओल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विशेष रणनीतिक साझेदारी को मज़बूत करने पर सहमति जताई थी। साथ ही, दोनों नेताओं ने दक्षिण कोरिया की हिंद-प्रशांत रणनीति और भारत की एक्ट ईस्ट नीति के बीच सामंजस्यपूर्ण सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता में योगदान जारी रखने का संकल्प लिया।
आर्थिक और व्यापार सहयोग में, दोनों पक्षों की बढ़ती चिंताओं को दूर करने के लिए सीईपीए में संशोधन हेतु वार्ता शुरू की गई है।
साथ ही, नई दिल्ली ने सियोल की तेजी से परिष्कृत होती जा रही हथियार प्रणालियों में रुचि व्यक्त की है, जिसके परिणामस्वरूप दक्षिण कोरिया के K9 स्व-चालित हॉवित्जर को भारत को निर्यात करने के लिए 650 मिलियन डॉलर का सौदा हुआ है, साथ ही दक्षिण एशियाई देश में हथियार प्रणालियों के निर्माण के लिए संभावित संयुक्त उद्यमों पर भी चर्चा हुई है।
बाधा का सामना करना
उपरोक्त उपलब्धियों के बावजूद, दोनों पक्षों को अभी भी कई दीर्घकालिक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
पहला, प्रयासों के बावजूद, दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे की माँगों पर रियायत देने की अनिच्छा के कारण सीईपीए संशोधन वार्ता गतिरोध में है। इस संदर्भ में, कुछ लोगों को चिंता है कि भारत और दक्षिण कोरिया 2030 तक 50 अरब डॉलर के व्यापार लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएँगे। भारत में दक्षिण कोरियाई निवेश भी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा है। भारत में पढ़ने वाले दक्षिण कोरियाई छात्रों की संख्या अभी भी कम है।
इसके अलावा, एक-दूसरे के प्रति धारणा सीमित है। भारत के कुछ हिस्सों में अभी भी मौजूद अस्वच्छ सार्वजनिक स्थलों, उच्च अपराध दर और सामाजिक असमानता की छवि दोनों देशों के बीच आर्थिक और रक्षा सहयोग पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। प्रति व्यक्ति आय में भारी अंतर, जिसमें दक्षिण कोरिया का आंकड़ा भारत से काफी अधिक है, दक्षिण एशियाई देश के प्रति पूर्वाग्रह को बढ़ावा देता है, जिससे साझेदारी की गतिशीलता प्रभावित होती है।
दूसरी ओर, अब समय आ गया है कि नई दिल्ली सियोल को सिर्फ़ निवेश, तकनीक हस्तांतरण और नए हथियारों की ख़रीद के स्रोत के रूप में न देखकर एक व्यापक साझेदार के रूप में देखे। चूँकि दक्षिण कोरिया आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें 2050 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में उसके 15वें स्थान पर गिरने का अनुमान भी शामिल है, इसलिए भारत को सियोल को आगे आने वाली चुनौतियों से निपटने में सहयोग देने के लिए एक व्यापक रणनीति की ज़रूरत है।
अंततः, रक्षा सहयोग के मामले में, दक्षिण कोरिया का रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन (डीएपीए) नई दिल्ली के साथ अपने व्यवहार में सतर्क रहा है। इसने दक्षिण कोरिया से उन्नत हथियार प्रणालियाँ खरीदने और दक्षिण कोरिया से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुनिश्चित करने के भारत के प्रयासों को बार-बार बाधित किया है, जिससे दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी को पूर्ण रूप से साकार करने में बाधा उत्पन्न हुई है।
उस समय, दोनों पक्षों को मनोवैज्ञानिक अंतर को कम करने, सतत विकास में योगदान देने और दुनिया के उतार-चढ़ाव के साथ तालमेल बिठाने की ज़रूरत है। यह अगले पाँच दशकों और उसके बाद भी भारत-कोरिया संबंधों के सतत विकास के लिए ज़रूरी है।
[विज्ञापन_2]
स्रोत




![[फोटो] राष्ट्रपति लुओंग कुओंग सैन्य क्षेत्र 3 के सशस्त्र बलों के पारंपरिक दिवस की 80वीं वर्षगांठ में शामिल हुए](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/28/1761635584312_ndo_br_1-jpg.webp)


























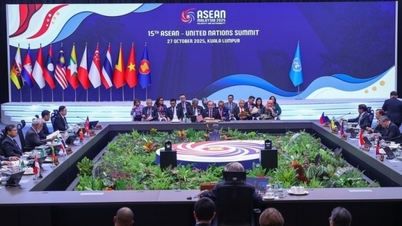



![[फोटो] नेशनल असेंबली के अध्यक्ष ट्रान थान मान उज़्बेकिस्तान के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नूरिद्दीन इस्माइलोव से मिलते हुए](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/27/1761542647910_bnd-2610-jpg.webp)
![[फोटो] केंद्रीय निरीक्षण आयोग की 5वीं देशभक्ति अनुकरण कांग्रेस](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/27/1761566862838_ndo_br_1-1858-jpg.webp)
![[फोटो] केंद्रीय पार्टी एजेंसियों की पार्टी समितियाँ संकल्प संख्या 18-एनक्यू/टीडब्ल्यू के कार्यान्वयन और पार्टी कांग्रेस की दिशा का सारांश प्रस्तुत करती हैं](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/27/1761545645968_ndo_br_1-jpg.webp)


















































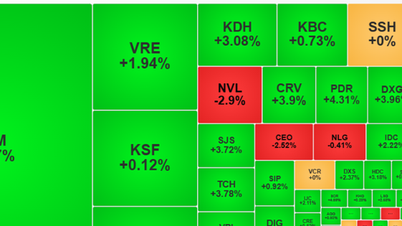






















टिप्पणी (0)