नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए आवश्यक धातुओं की आपूर्ति पर दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि देश 2050 तक कार्बन तटस्थ बनने की होड़ में लगे हैं।
हाल के महीनों में, ब्रिटेन ने ज़ाम्बिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जापान ने नामीबिया के साथ साझेदारी की है, और यूरोपीय संघ ने चिली के साथ हाथ मिलाया है। यूरोपीय संघ के वार्ताकारों ने कांगो के साथ भी काम करना शुरू कर दिया है, जबकि अमेरिका मंगोलिया की ओर देख रहा है। इन प्रयासों का लक्ष्य डीकार्बोनाइज़ेशन, या "हरित" धातुओं के लिए आवश्यक खनिजों की आपूर्ति करना है।
"हरित" धातुओं के तीन समूह हैं जिनका कई उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है: एल्युमीनियम और स्टील का उपयोग सौर पैनल और टर्बाइन बनाने में किया जाता है, जबकि तांबा केबल से लेकर कारों तक, हर चीज़ के लिए महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों में इस्तेमाल होने वाले समूह में कोबाल्ट, लिथियम और निकल शामिल हैं, जो कैथोड बनाते हैं, और ग्रेफाइट, जो एनोड का मुख्य घटक है। अंतिम समूह चुंबकीय दुर्लभ मृदाएँ हैं, जैसे नियोडिमियम, जिनका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों की मोटरों और टर्बाइन जनरेटरों में किया जाता है, और जिनकी माँग कम है।
ऊर्जा संक्रमण आयोग (ईटीसी) परामर्श के अनुसार, 72 देशों, जो वैश्विक उत्सर्जन के 4/5वें हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं, ने 2050 तक कार्बन तटस्थता के लिए प्रतिबद्धता जताई है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, पवन ऊर्जा क्षमता में 15 गुना, सौर ऊर्जा में 25 गुना, ग्रिड अवसंरचना में 3 गुना वृद्धि तथा इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में 60 गुना वृद्धि करनी होगी।
2030 तक, तांबे और निकल की मांग 50-70%, कोबाल्ट और नियोडिमियम की मांग 150%, और ग्रेफाइट और लिथियम की मांग छह से सात गुना बढ़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, 2050 तक कार्बन-तटस्थ दुनिया को कुल मिलाकर प्रति वर्ष 35 मिलियन टन "हरित धातुओं" की आवश्यकता होगी। यदि आप इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक पारंपरिक धातुओं, जैसे एल्युमीनियम और स्टील, को भी शामिल कर लें, तो अब और तब के बीच मांग 6.5 बिलियन टन होगी।
यही कारण है कि देश इस दशक के अंत तक वैश्विक खनिज आपूर्ति की पूर्ण कमी को लेकर चिंतित हैं। ईटीसी को 2030 तक तांबे और निकल की लगभग 10-15% और बैटरियों में इस्तेमाल होने वाली अन्य धातुओं की 30-45% कमी का अनुमान है।
तो इन धातुओं की आपूर्ति का क्या? स्टील शायद प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहेगा। कोबाल्ट भी प्रचुर मात्रा में है। लेकिन इकोनॉमिस्ट द्वारा प्रकाशित विशेषज्ञों के पूर्वानुमानों के अनुसार, 2030 तक तांबे की आपूर्ति 20-40 लाख टन या संभावित मांग के 6-15% तक कम होगी। लिथियम की आपूर्ति 50,000-100,000 टन या मांग के 2-4% तक कम होगी। निकल और ग्रेफाइट सैद्धांतिक रूप से प्रचुर मात्रा में हैं, लेकिन बैटरियों के लिए उच्च शुद्धता की आवश्यकता होती है। बॉक्साइट को एल्युमीनियम में परिशोधित करने के लिए बहुत कम प्रगालक हैं। और चीन के बाहर शायद ही कोई नियोडिमियम बनाता हो।
द इकोनॉमिस्ट इन चुनौतियों के तीन समाधान सुझाता है। पहला, उत्पादक मौजूदा खदानों से अधिक आपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं, जो तुरंत किया जा सकता है, लेकिन अतिरिक्त उत्पादन सीमित होगा। दूसरा, कंपनियाँ नई खदानें खोल सकती हैं, जिससे समस्या पूरी तरह हल हो सकती है, लेकिन इसमें लंबा समय लगता है।
ये सीमाएँ तीसरे समाधान को, कम से कम अगले दशक में, सबसे महत्वपूर्ण बनाती हैं। यानी "हरित बाधाओं" को दूर करने के तरीके खोजना। इनमें ज़्यादा सामग्रियों का पुन: उपयोग शामिल है, जो एल्युमीनियम, तांबे और निकल के मामले में सबसे ज़्यादा संभव है। रीसाइक्लिंग उद्योग अभी भी बिखरा हुआ है और अगर कीमतें ज़्यादा होतीं, तो यह बढ़ सकता था। कुछ प्रयास पहले से ही चल रहे हैं, जैसे कि खनन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एचपी द्वारा तंजानिया में एक निकल रीसाइक्लिंग स्टार्टअप को वित्त पोषित करना।
एचपी के मुख्य अर्थशास्त्री ह्यू मैके का अनुमान है कि एक दशक में कुल तांबे की आपूर्ति में स्क्रैप का हिस्सा 50% हो सकता है, जो आज 35% है। रियो टिंटो एल्युमीनियम रीसाइक्लिंग केंद्रों में भी निवेश कर रही है। पिछले साल, बैटरी-धातु रीसाइक्लिंग स्टार्टअप्स ने रिकॉर्ड 50 करोड़ डॉलर जुटाए।
बड़ा रास्ता बंद पड़ी खदानों को फिर से शुरू करना है, जिसमें एल्युमीनियम सबसे आशाजनक है। दिसंबर 2021 से, बढ़ती ऊर्जा लागत ने यूरोप में 14 लाख टन वार्षिक एल्युमीनियम गलाने की क्षमता (दुनिया की 2%) को बंद कर दिया है। कमोडिटी ट्रेडर ट्रैफिगुरा के मुख्य धातु एवं खनिज विश्लेषक ग्रीम ट्रेन के अनुसार, एल्युमीनियम की कीमतों में 25% की वृद्धि से और अधिक खदानें फिर से खुलेंगी।
और सबसे बड़ी उम्मीद उन तकनीकों में है जो दुर्लभ आपूर्ति का अधिकतम लाभ उठाती हैं। कंपनियाँ "टेल लीचिंग" नामक प्रक्रियाएँ विकसित कर रही हैं, जो कम धातु सामग्री वाले अयस्कों से तांबा निकालती हैं। अमेरिकी संसाधन प्रौद्योगिकी कंपनी जेटी रिसोर्सेज के बोर्ड सदस्य डैनियल मालचुक के अनुसार, इस तकनीक का बड़े पैमाने पर उपयोग करके कम लागत पर प्रति वर्ष अतिरिक्त 10 लाख टन तांबा उत्पादित किया जा सकता है।

इंडोनेशिया के दक्षिण सुलावेसी प्रांत में एक निकल प्रसंस्करण संयंत्र में काम करता एक कर्मचारी। फोटो: रॉयटर्स
दुनिया के सबसे बड़े निकल उत्पादक इंडोनेशिया में, खनिक निम्न-श्रेणी के अयस्क को इलेक्ट्रिक कारों के लिए उपयुक्त सामग्री में बदलने के लिए "उच्च-दाब एसिड लीचिंग" नामक प्रक्रिया का उपयोग कर रहे हैं। तीन अरबों डॉलर के संयंत्र बनाए गए हैं, और लगभग 20 अरब डॉलर की अतिरिक्त परियोजनाओं की घोषणा की गई है।
ब्रिटेन की वित्तीय फर्म सुकडेन में अनुसंधान प्रमुख डारिया एफानोवा का अनुमान है कि इंडोनेशिया 2030 तक लगभग 400,000 टन उच्च-श्रेणी निकल का उत्पादन कर सकता है, जो अनुमानित 900,000 टन आपूर्ति अंतर को आंशिक रूप से पूरा कर देगा।
लेकिन नई तकनीकें अभी भी अनिश्चित हैं और प्रदूषण जैसी कमियाँ भी हो सकती हैं। इसलिए नई खदानें खोलने से ज़्यादा मुनाफ़ा होगा, भले ही इसमें समय लगे। दुनिया भर में 382 कोबाल्ट, तांबा, लिथियम और निकल परियोजनाएँ हैं जिनके कम से कम पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन शुरू हो चुके हैं। कंसल्टिंग फर्म मैकिन्से के अनुसार, अगर ये 2030 तक चालू हो जाती हैं, तो ये माँग को संतुलित कर सकती हैं।
वर्तमान में दुनिया भर में लगभग 500 कोबाल्ट, तांबा, लिथियम और निकल खदानें चल रही हैं। 382 नई खदानों को समय पर चालू करने के लिए कई बाधाओं को पार करना होगा। पहली चुनौती धन की कमी है। मैकिन्से के अनुसार, 2030 तक आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए, खनन में वार्षिक पूंजीगत व्यय को दोगुना करके 300 अरब डॉलर करना होगा।
कंसल्टिंग फर्म सीआरयू का कहना है कि अकेले तांबे पर खर्च 2027 तक 22 अरब डॉलर तक पहुँच जाएगा, जो 2016 और 2021 के बीच औसतन 15 अरब डॉलर था। प्रमुख खनिकों द्वारा निवेश बढ़ रहा है, लेकिन पर्याप्त तेज़ी से नहीं। इसके अलावा, नई खदानों के विकास में काफ़ी समय लगता है, लिथियम के लिए चार से सात साल और तांबे के लिए औसतन 17 साल। परमिट की कमी के कारण यह देरी और भी लंबी हो सकती है।
चूंकि कार्यकर्ता, सरकारें और नियामक पर्यावरणीय आधार पर परियोजनाओं को तेजी से अवरुद्ध कर रहे हैं, इसलिए चिली में नई खदानों को मंजूरी देने में 2017 और 2021 के बीच औसतन 311 दिन लगे, जबकि 2002 और 2006 के बीच 139 दिन लगे थे।
अधिक अनुकूल देशों में खनन किए गए तांबे के अयस्क में धातु की मात्रा कम हो रही है, जिससे कंपनियों को कठिन स्थानों की ओर रुख करना पड़ रहा है। 2030 तक अपेक्षित नई आपूर्ति का दो-तिहाई हिस्सा विश्व बैंक के "व्यापार करने में आसानी" सूचकांक में सबसे निचले 50 देशों में होगा।
इसका मतलब यह है कि नई आपूर्ति ही दीर्घकालिक समाधान हो सकती है। इसलिए अगले दशक में होने वाला ज़्यादातर समायोजन इनपुट बचत पर निर्भर करेगा। लेकिन यह कितना होगा, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि यह विनिर्माण कंपनियों की नवाचार करने की क्षमता पर निर्भर करता है।
उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रिक कार और बैटरी निर्माताओं ने कम धातु का उपयोग करके प्रगति की है। एक सामान्य इलेक्ट्रिक कार बैटरी में अब केवल 69 किलोग्राम तांबा होता है, जो 2020 में 80 किलोग्राम था। सीआरयू में प्राथमिक धातुओं के प्रमुख साइमन मॉरिस का अनुमान है कि अगली पीढ़ी की बैटरियों को केवल 21-50 किलोग्राम तांबे की आवश्यकता हो सकती है, जिससे 2035 तक प्रति वर्ष 20 लाख टन तांबे की बचत होगी। बैटरियों में लिथियम की मांग भी 2027 तक आधी हो सकती है।
बचत और विकल्पों के अलावा, बैटरी कैथोड में, निकल-मैंगनीज-कोबाल्ट रसायन, जिनमें कोबाल्ट और निकल की समान मात्रा होती है, जिन्हें NMC 111 के नाम से जाना जाता है, को धीरे-धीरे NMC 721 और 811 के पक्ष में हटाया जा रहा है, जिनमें निकल ज़्यादा होता है लेकिन कोबाल्ट कम होता है। इस बीच, चीन में सस्ते लेकिन कम ऊर्जा खपत वाले लिथियम-आयरन फ़ॉस्फ़ेट (LFP) मिश्रण लोकप्रिय हैं, जहाँ शहरी निवासियों को एक बार चार्ज करने पर लंबी दूरी तय करने की ज़रूरत नहीं होती।
ग्रेफाइट एनोड्स को सिलिकॉन (जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है) से भी डोप किया जा रहा है। टेस्ला का कहना है कि वह दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के बिना मोटर बनाएगी। लिथियम की जगह सोडियम (पृथ्वी पर छठा सबसे प्रचुर तत्व) का उपयोग करने वाली सोडियम-आयन बैटरियाँ सफल हो सकती हैं।
उपभोक्ता की पसंद भी एक भूमिका निभाएगी। आज, लोग चाहते हैं कि उनकी इलेक्ट्रिक कारें एक बार चार्ज करने पर 600 किलोमीटर चलें, लेकिन बहुत कम लोग नियमित रूप से इतनी लंबी यात्राएँ करते हैं। लिथियम की आपूर्ति कम होने के कारण, वाहन निर्माता कम दूरी की कारें, अदला-बदली योग्य बैटरियों के साथ डिज़ाइन कर सकते हैं, जिससे बैटरी का आकार काफ़ी कम हो जाएगा। सही कीमत के साथ, इसे तेज़ी से अपनाया जा सकता है।
मुख्य चुनौती तांबा है, जिसे ग्रिड से हटाना आसान नहीं है। लेकिन उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव से मदद मिल सकती है। सीआरयू का अनुमान है कि "हरित" उद्देश्यों के लिए तांबे की मांग आज के 7% से बढ़कर 2030 तक 21% हो जाएगी। जैसे-जैसे धातुओं की कीमतें बढ़ेंगी, तांबे से बने फोन और वाशिंग मशीनों की बिक्री बिजली के तारों और सौर पैनलों की तुलना में जल्दी घट सकती है, खासकर अगर हरित प्रौद्योगिकी बाजार को सरकारें सब्सिडी देती हैं।
2030 के दशक के अंत तक, पर्याप्त नई खदानें और पुनर्चक्रण क्षमताएँ उपलब्ध हो सकती हैं ताकि हरित परिवर्तन योजना के अनुसार आगे बढ़ सके। लेकिन इकोनॉमिस्ट के अनुसार, जोखिम अन्य व्यवधानों में भी निहित है।
चूँकि आपूर्ति कुछ ही देशों तक सीमित है, इसलिए स्थानीय अशांति, भू-राजनीतिक संघर्ष या यहाँ तक कि खराब मौसम भी इस पर असर डाल सकता है। पेरू में खनिकों की हड़ताल या इंडोनेशिया में तीन महीने का सूखा कीमतों को प्रभावित कर सकता है या तांबे और निकल की आपूर्ति को 5-15% तक कम कर सकता है। लेकिन लिबरम कैपिटल (यूके) के सिमुलेशन के अनुसार, लचीले खरीदारों, मज़बूत सरकारों और थोड़ी किस्मत के साथ, "हरित" धातुओं की बढ़ती माँग विनाशकारी गिरावट का कारण नहीं बन सकती है।
फिएन एन ( द इकोनॉमिस्ट के अनुसार )
[विज्ञापन_2]
स्रोत लिंक


![[फोटो] हो ची मिन्ह सिटी के युवा स्वच्छ पर्यावरण के लिए कदम उठाते हुए](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/04/1762233574890_550816358-1108586934787014-6430522970717297480-n-1-jpg.webp)
![[फोटो] डोंग नाई को हो ची मिन्ह सिटी से जोड़ने वाली सड़क निर्माण के 5 साल बाद भी अधूरी है।](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/04/1762241675985_ndo_br_dji-20251104104418-0635-d-resize-1295-jpg.webp)

![[फोटो] 2025-2030 की अवधि के लिए नहान दान समाचार पत्र की देशभक्ति अनुकरण कांग्रेस का पैनोरमा](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/04/1762252775462_ndo_br_dhthiduayeuncbaond-6125-jpg.webp)

![[फोटो] का माऊ वर्ष के सबसे ऊंचे ज्वार से निपटने के लिए "संघर्ष" कर रहा है, अलर्ट स्तर 3 को पार करने का अनुमान है](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/04/1762235371445_ndo_br_trieu-cuong-2-6486-jpg.webp)












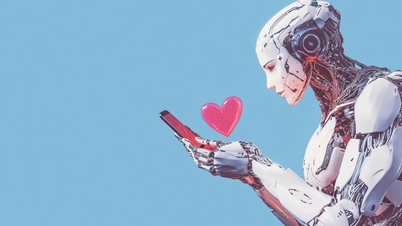























































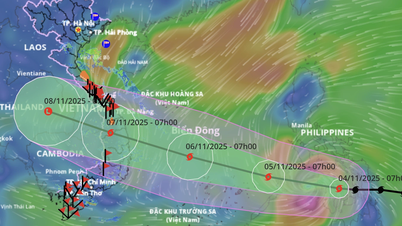




























टिप्पणी (0)