बच्चों की "बुरी आदतें" उच्च IQ का संकेत हो सकती हैं। हालाँकि माता-पिता चिंतित और निराश हो जाते हैं, लेकिन कई व्यवहार जिन्हें वयस्क अनुचित मानते हैं, वे वास्तव में बच्चे की रचनात्मकता, कल्पनाशीलता और सोचने की क्षमता को दर्शाते हैं।
चीनी मनोवैज्ञानिक संघ की कानूनी मनोविज्ञान व्यावसायिक समिति के उप निदेशक और प्रसिद्ध मनोविज्ञान प्रोफेसर ली मीजिन के अनुसार, कुछ बच्चे जो "गुस्सैल" लगते हैं, वास्तव में उनका आईक्यू उच्च होता है। माता-पिता को उन्हें डाँटने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे उनका आंतरिक उत्साह नष्ट हो सकता है और उनके मस्तिष्क के विकास पर असर पड़ सकता है।
इस बीच, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में न्यूरोलॉजी के प्रोफेसर मेयर ने भी कहा कि उच्च आईक्यू वाले बच्चे अक्सर 6 साल की उम्र से पहले ही कुछ सामान्य विशेषताएँ दिखाते हैं। अगर माता-पिता उनका सही मार्गदर्शन करें, तो उनके बच्चों का आईक्यू काफ़ी बढ़ सकता है। हालाँकि, कई माता-पिता इस बात को समझ नहीं पाते, इसलिए वे अनजाने में अपने बच्चों के बौद्धिक विकास में बाधा डालते हैं।
बच्चे बहुत ज़्यादा बोलते हैं
बातूनी बच्चे अक्सर बहिर्मुखी, आशावादी होते हैं और उनकी भाषा कौशल अच्छी होती है। वे बातचीत करने में आत्मविश्वासी होते हैं और दोस्तों से आसानी से जुड़ सकते हैं। अक्सर वे ही बातचीत की शुरुआत करते हैं, जिससे कक्षा में एक मज़ेदार और दोस्ताना माहौल बनता है।

हालाँकि, इस जीवंतता के कारण बच्चों के लिए खुद पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो सकता है। बात बस इतनी है कि बच्चे अस्थायी रूप से आत्म-नियंत्रण में अच्छे नहीं होते, अपनी बात करने की इच्छा पर नियंत्रण नहीं रख पाते, इसलिए बोलते रहते हैं। इससे बच्चे व्याख्यान पर ध्यान नहीं दे पाते, जिससे उनकी एकाग्रता भंग हो जाती है। इससे कई माता-पिता परेशान हो जाते हैं।
यद्यपि बातूनी बच्चों ने बेहतर भाषा कौशल का प्रदर्शन किया है, फिर भी उन्हें परिस्थितियों का आकलन करना तथा यह जानना भी सिखाया जाना चाहिए कि कब बोलना है और कब नहीं, ताकि दूसरों को बोर या परेशान न किया जा सके।
बेशक, माता-पिता को अपने बच्चों की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए और उन्हें खुशी से बात करने देना चाहिए। बच्चों के लिए एक अच्छा भाषाई वातावरण बनाएँ ताकि वे अधिक विनम्रता से बोल सकें। अंत में, माता-पिता अपने बच्चों के ज्ञान का विस्तार कर सकते हैं और उनकी तार्किक क्षमता में सुधार कर सकते हैं, उन्हें पढ़ने, दूसरों से बात करने, बहस करने आदि का मौका देकर, ताकि उनकी बातचीत अधिक आकर्षक और तार्किक हो।
जिद्दी और सलाह सुनने को तैयार नहीं
हर बच्चे का अपना व्यक्तित्व होता है। मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के अनुसार, ज़िद्दी और अवज्ञाकारी बच्चे ज़्यादातर गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। ये बच्चे बहुत स्वतंत्र होते हैं और इनके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं। माता-पिता अपने बच्चों को अपनी इच्छानुसार विकास करने के लिए सीधे तौर पर मजबूर नहीं कर सकते।
माता-पिता को पहले खुद को सही स्थिति में रखना चाहिए और अपने बच्चों पर ऊँची स्थिति से हुक्म नहीं चलाना चाहिए। इससे बच्चे और ज़्यादा विद्रोही हो जाएँगे। माता-पिता अपने बच्चों से दोस्त की तरह बात कर सकते हैं और उनकी इच्छाओं का सम्मान कर सकते हैं।
या खिलौनों को नष्ट करें, चीजें फेंकें
जब बच्चे एक खास उम्र में पहुँच जाते हैं, तो उन्हें अचानक खिलौने तोड़ने और चीज़ें फेंकने का बहुत शौक हो जाता है। अगर माता-पिता उन्हें ऐसा करने से रोकें, तो वे और भी ज़ोर से फेंकेंगे। कई बार, माता-पिता घर में "हर जगह गंदगी" देखते हैं, यहाँ तक कि नया खरीदा हुआ खिलौना भी टूटा हुआ होता है, तो वे गुस्सा होने से खुद को नहीं रोक पाते।

प्रोफेसर मेयर का मानना है कि माता-पिता को बच्चों को चीजों को अलग-अलग करने और फेंकने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि यह वास्तव में अन्वेषण का एक महत्वपूर्ण सबक है, बच्चे जागरूकता बढ़ाने और जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं।
तोड़ने और फेंकने की क्रिया के माध्यम से, बच्चे सीखते हैं कि वस्तुओं की बनावट और वज़न अलग-अलग होते हैं। जब वे ज़मीन पर गिरती हैं, तो वे अलग-अलग आवाज़ें, आकृतियाँ बनाती हैं और अलग-अलग दिशाओं में जाती हैं। इस क्रिया को पूरा करने के लिए, बच्चों की आँखों, दिमाग, हाथों आदि को एक-दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर अच्छे शारीरिक समन्वय का अभ्यास करना ज़रूरी है।
खासकर 1 से 3 साल की उम्र में, बच्चे "नष्ट-कर्म" करके दुनिया के बारे में सीख रहे होते हैं। इसलिए, माता-पिता को अपने बच्चों के शरारती होने पर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस तरह से उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं।
सबसे पहले, अपने बच्चे को गंदगी खुद साफ़ करने दें। दूसरा, माता-पिता अपने बच्चों की गतिविधियों में भाग ले सकते हैं, जैसे कि जब वे किसी चीज़ को अलग-अलग करते हैं। इस प्रक्रिया में, माता-पिता को अपने बच्चों से सवाल पूछने चाहिए, उनकी सोचने की क्षमता को बढ़ावा देना चाहिए और उनकी सोचने की क्षमता में सुधार करना चाहिए।
बेशक, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माता-पिता को स्वयं एक अच्छा रवैया बनाए रखना चाहिए और अपने बच्चों को "विनाश" के लिए डांटना नहीं चाहिए, अन्यथा यह उनकी खोज करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न करेगा और बच्चों को धीरे-धीरे अपने आसपास की दुनिया के बारे में अपनी जिज्ञासा खोने का कारण बनेगा।
चंचल, माता-पिता बुलाते हैं लेकिन परवाह नहीं करते
कई माता-पिता अपने बच्चों को खेलते देखकर निराश हो जाते हैं, यहाँ तक कि उन्हें याद भी दिलाते हैं, लेकिन बच्चे अनसुना कर देते हैं। लेकिन असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एकाग्र होते हैं। जब बच्चे खेल रहे हों या कोई भी गतिविधि कर रहे हों, जैसे पढ़ना, चित्र बनाना,... तो माता-पिता को उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए।
एकाग्रता एक ठोस आधार है जो लोगों को अपना भविष्य बनाने के लिए प्रेरित करती है। अपने बच्चों को कोशिश करने दें, जब वे ध्यान लगा रहे हों तो उन्हें बीच में न रोकें। अगर माता-पिता देखते हैं कि उनके बच्चे खेलने में बहुत ज़्यादा मग्न हैं, तो आप समय को सीमित कर सकते हैं, साथ ही खेलों पर निर्भरता कम करने के लिए एकाग्रता सुनिश्चित कर सकते हैं।

दूसरे लोग जो कहते हैं उसे दोहराना पसंद करते हैं
कुछ बच्चे हमेशा वही दोहराते रहते हैं जो दूसरों ने अभी-अभी कहा है या जो विज्ञापन उन्होंने अभी-अभी देखे हैं। माता-पिता को लग सकता है कि उनके बच्चे नए विचारों वाले नहीं हैं और इसलिए वे हमेशा वही दोहराते हैं जो दूसरों ने कहा है।
लेकिन इसे दूसरे तरीके से सोचें, बच्चे की इन शब्दों को दोहराने की क्षमता सिर्फ़ यही दर्शाती है कि उसकी याददाश्त कमाल की है। और जैसे-जैसे वह दूसरों के शब्दों को दोहराता रहता है, उसकी याददाश्त और भी बेहतर होती जाती है।
माता-पिता को अपने बच्चों को ऐसा करने से रोकने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें शब्दों को दोहराने के बाद उनके विचारों और समझ को व्यक्त करने के लिए मार्गदर्शन दे सकते हैं। इससे न केवल उनकी स्मरण शक्ति का विकास होता है, बल्कि उनकी सोचने की क्षमता भी बेहतर होती है।
[विज्ञापन_2]
स्रोत: https://giadinhonline.vn/tre-co-iq-cao-mang-5-tat-xau-khi-con-nho-khong-it-cha-me-buc-minh-d203253.html


![[फोटो] केंद्रीय आंतरिक मामलों के आयोग की तीसरी देशभक्ति अनुकरण कांग्रेस](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/30/1761831176178_dh-thi-dua-yeu-nuoc-5076-2710-jpg.webp)
![[फोटो] हज़ारों लोगों द्वारा तटबंध को उफनते पानी से बचाने का मार्मिक दृश्य](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/30/1761825173837_ndo_br_ho-de-3-jpg.webp)
![[फोटो] महासचिव टो लैम वियतनाम-यूके उच्च-स्तरीय आर्थिक सम्मेलन में भाग लेते हुए](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/30/1761825773922_anh-1-3371-jpg.webp)

![[फोटो] नेशनल असेंबली के अध्यक्ष ट्रान थान मान ने अलविदा कहने आए विदेशी राजदूतों का स्वागत किया](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/30/1761820977744_ndo_br_1-jpg.webp)
![[फोटो] महासचिव टू लैम ने पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर से मुलाकात की](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/30/1761821573624_tbt-tl1-jpg.webp)









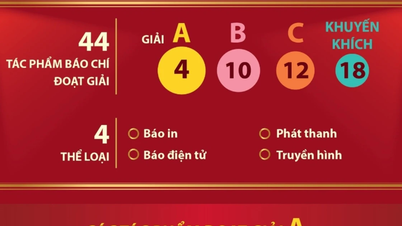

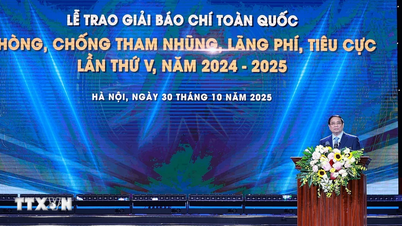



































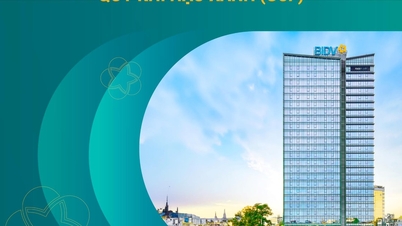



















































टिप्पणी (0)