यूक्रेन में संघर्ष लगभग दो साल से चल रहा है। गाजा पट्टी में इज़राइल और हमास के बीच लड़ाई दो महीने से चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संबंधित देशों के लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है: यह युद्ध कब और किस रूप में समाप्त होगा?
 |
| संघर्षों और युद्धों को समाप्त करने, सभी पक्षों के नुकसान को कम करने और विश्व शांति के लिए बातचीत एक महत्वपूर्ण समाधान है, लेकिन इसकी शुरुआत और प्रक्रिया बहुत कठिन और जटिल है। (स्रोत: गेटी इमेजेज़) |
बातचीत जटिल होती है और कई कारकों पर निर्भर करती है।
अतीत में, युद्ध अक्सर "ब्लैकआउट" में समाप्त होते थे, जिसमें एक पक्ष पराजित हो जाता था, युद्ध जारी रखने में असमर्थ हो जाता था, राजनीतिक व्यवस्थाओं में बदलाव स्वीकार कर लेता था, और उसके क्षेत्र विभाजित हो जाते थे। हाल के दशकों में, युद्धों के अंत में बातचीत के उदाहरण सामने आए हैं। बातचीत क्यों और किन परिस्थितियों में होती है?
सबसे पहले , युद्ध के नए प्रकार सामने आए हैं, जिनके जटिल विकास और परिणाम हैं जिनकी भविष्यवाणी करना मुश्किल है। अपरंपरागत युद्ध, छद्म युद्ध, जटिल युद्ध आदि जैसे नए प्रकारों में, गैर- सैन्य गतिविधियों (आर्थिक, कूटनीतिक, सांस्कृतिक, सूचना और संचार, आदि) की भूमिका और प्रभाव लगातार महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। कमज़ोर पक्ष "असममित" चालें और उपाय अपना सकता है, जिससे कुल शक्ति का अंतर कम हो जाता है, युद्ध गतिरोध में आ जाता है और लंबा खिंच जाता है। मज़बूत पक्ष कम समय में आसानी से जीत नहीं सकता, और यहाँ तक कि लड़खड़ा भी सकता है। वह जीत तो सकता है, लेकिन फिर युद्ध फिर से छिड़ जाता है।
बाहरी कारकों की भागीदारी और प्रभाव शक्ति संतुलन और संघर्ष की स्थिति को तेज़ी से प्रभावित कर रहे हैं। पश्चिमी सहायता, हथियार, वित्तीय, राजनीतिक, कूटनीतिक समर्थन... यूक्रेन के लिए बचाव और जवाबी हमले करने और युद्ध के मैदान में स्थिति को पलटने के लिए अपरिहार्य कारक हैं। हमास को सशस्त्र इस्लामी संगठनों हिज़्बुल्लाह, हूती और ईरान से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त होता है... ताकि इज़राइल के साथ शक्ति के अंतर को कुछ हद तक कम किया जा सके और एक स्वीकार्य परिणाम प्राप्त किया जा सके।
ये कारक संघर्ष को आसानी से लम्बा खींच देते हैं, संभवतः उसे उलझा देते हैं, अप्रत्याशित घटनाक्रम और परिणाम उत्पन्न करते हैं, जिससे पक्षकारों को अन्य विकल्पों पर विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ता है।
दूसरा , कई देशों और क्षेत्रों में इसके भयावह और बहुआयामी प्रभावों को मापना मुश्किल है। सभी पक्षों को सैन्य, राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक नुकसान आदि हो सकते हैं; बड़ी संख्या में नागरिक मारे जाएँगे, बुनियादी ढाँचा नष्ट हो जाएगा, जिसके कई पीढ़ियों तक गंभीर आर्थिक और सामाजिक परिणाम होंगे।
युद्ध में सीधे तौर पर शामिल देश ही नहीं, बल्कि पूरा क्षेत्र और पूरी दुनिया प्रभावित होती है। प्रतिबंध और नाकेबंदी कई देशों को पक्ष चुनने के लिए मजबूर करती हैं, जिससे विभाजन होता है, संसाधन बिखरते हैं, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित होती है और आर्थिक मंदी आती है। शरणार्थियों और प्रवासियों की आमद कई देशों में सामाजिक अस्थिरता पैदा करती है।
संघर्ष जितना लंबा चलेगा, उसका नकारात्मक प्रभाव उतना ही ज़्यादा होगा। सूचना और संचार के विकास से दुनिया को युद्ध के परिणामों का एहसास ज़्यादा तेज़ी से, सहज रूप से, स्पष्ट रूप से और स्पष्टता से होता है। यह नेताओं को संघर्षों से जुड़े फ़ैसलों पर गंभीरता से विचार करने के लिए मजबूर करता है।
तीसरा , इसके बहुआयामी परिणाम युद्ध-विरोधी आंदोलन को बढ़ावा देते हैं, युद्धरत और युद्धरत देशों, क्षेत्र और दुनिया भर के कई अन्य देशों में युद्धविराम और शांति वार्ता की मांग करते हैं। इससे सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, खासकर युद्ध में सीधे तौर पर शामिल पक्षों पर, भारी दबाव बनता है। यह माँग करते हुए कि पक्ष युद्धविराम, वार्ता और संघर्ष को समाप्त करने के लिए समाधान खोजने की दिशा में कार्रवाई करें।
प्रमुख शक्तियाँ वार्ता को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हालाँकि, यह तथ्य कि कुछ प्रमुख शक्तियाँ युद्ध का लाभ उठाकर अपने विरोधियों को कमज़ोर करती हैं, अन्य देशों को उन पर निर्भर रहने के लिए मजबूर करती हैं, और प्रभाव तथा रणनीतिक स्थिति के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं, वार्ता द्वारा समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा।
चौथा, यह मुश्किल है , लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी है। बातचीत करने की क्षमता और बातचीत की प्रक्रिया कई कारकों पर निर्भर करती है, आंतरिक और बाह्य, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपरक दोनों। पक्षों की शक्ति, उद्देश्य, लक्ष्य, रणनीति और कार्यनीति का सहसंबंध ही प्रत्यक्ष निर्णायक कारक है। लक्ष्य जितने ऊँचे और परस्पर विरोधी होंगे, बातचीत करने की क्षमता उतनी ही कम होगी और बातचीत की प्रक्रिया उतनी ही जटिल और लंबी होगी।
सबसे मुश्किल बात यह है कि दोनों पक्षों की स्थितियाँ बहुत अलग-अलग हैं, यहाँ तक कि विरोधी भी। कमज़ोर पक्ष अक्सर बातचीत करना चाहता है, लेकिन कोशिश करता है कि ज़्यादा नुकसान न हो। मज़बूत पक्ष पूरी तरह से जीतना चाहता है; वह बातचीत तभी स्वीकार करता है जब उसे भारी नुकसान हो, कड़े विरोध का सामना करना पड़े, कम समय में जीतना मुश्किल हो, और फंसने का ख़तरा हो।
| सबसे कठिन बात यह है कि दोनों पक्षों की स्थिति बहुत अलग-अलग है, यहां तक कि एक-दूसरे के विपरीत भी है। |
बातचीत का उद्देश्य संघर्षों को सबसे लाभकारी तरीके से समाप्त करना होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल सेनाओं को एकजुट करने, प्रतिद्वंद्वी के हमले की गति को सीमित करने, या घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से निपटने के लिए समय हासिल करने के लिए भी किया जा सकता है। बातचीत की प्रक्रिया को सैन्य गतिविधियों के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे प्रतिद्वंद्वी पर दबाव डाला जा सकता है और उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा सकता है।
युद्धरत देशों में, या सीधे तौर पर शामिल प्रमुख देशों में, राजनीतिक परिवर्तन, वार्ता की संभावना और प्रगति को प्रभावित कर सकते हैं। यदि गैर-सैन्य तरीकों से संघर्षों को सुलझाने का पक्षधर पक्ष सत्ता में आता है, तो वार्ता को बढ़ावा मिलने की संभावना अधिक होती है, और इसके विपरीत।
इस प्रकार, संघर्षों को समाप्त करने, सभी पक्षों के नुकसान को कम करने और विश्व शांति के लिए बातचीत एक महत्वपूर्ण समाधान है, लेकिन इसकी शुरुआत और प्रक्रिया बहुत कठिन और जटिल है। सामान्य कारकों के अलावा, विकास प्रत्येक युद्ध की विशिष्ट स्थिति पर भी निर्भर करता है।
 |
| राजधानी कीव के स्वतंत्रता चौक पर रूस के साथ संघर्ष में मारे गए यूक्रेनी सैनिकों का स्मारक। (स्रोत: एपी) |
यूक्रेन में बातचीत अभी भी बहुत दूर है।
अब तक, रूस ने मूलतः क्रीमिया को अपने पास रखा है, दोनों अलगाववादी स्वायत्त गणराज्यों के क्षेत्रों पर कब्ज़ा कर लिया है और कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों का विस्तार किया है; आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता नहीं आई है; यूक्रेन की सैन्य और आर्थिक क्षमता का एक हिस्सा समाप्त हो गया है... लेकिन यूक्रेन में विसैन्यीकरण और तटस्थता का लक्ष्य मूलतः प्राप्त नहीं हुआ है। रूस को भी काफ़ी नुकसान हुआ है और उसके काफ़ी संसाधन ख़र्च हुए हैं।
रूसी क्षेत्र में गहरे ठिकानों पर हुए हमलों ने, जिससे भौतिक क्षति हुई, रक्षा प्रणाली की सीमाओं को उजागर किया और लोगों के मनोविज्ञान और भावना पर एक निश्चित प्रभाव डाला। रूस और यूरोपीय संघ के बीच संबंध लगभग स्थिर हो गए हैं। कभी सोवियत संघ और वारसॉ संधि के सदस्य रहे देशों और रूस के बीच संघर्ष लगातार गहराते जा रहे हैं। मध्य एशिया और काकेशस में रूस के कुछ घनिष्ठ सहयोगी पश्चिम की ओर झुकाव रखते हैं।
रूस कब्जे वाले इलाकों पर नियंत्रण और कुछ महत्वपूर्ण ठिकानों तक विस्तार की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन के अधिकांश हिस्सों में बड़े पैमाने पर आक्रमण करना, जिसके लिए बड़ी संख्या में सेनाओं की तैनाती की आवश्यकता होगी, रूस के लिए हालात और मुश्किल बना सकता है। युद्ध को जारी रखना, यूक्रेन में राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल पैदा करने वाले कारकों को उत्तेजित करना और कीव को शर्तें मानने के लिए मजबूर करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन इस बात की संभावना कम नहीं है कि मास्को फंस जाएगा और पश्चिम के इरादों में फँस जाएगा।
यूक्रेन का जवाबी हमला अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में काफ़ी हद तक विफल रहा है। कुछ सैन्य जनरलों और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की सरकार के बीच, और कुछ यूरोपीय संघ के देशों और यूक्रेन के बीच आंतरिक मतभेद के संकेत मिल रहे हैं। पश्चिमी देश अभी भी यूक्रेन को हथियार और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन धीमी गति से। ऐसे संकेत हैं कि कुछ देश चाहते हैं कि यूक्रेन रूस के साथ बातचीत करे और मध्यस्थ की भूमिका निभाने को तैयार हैं। हालाँकि, यूक्रेन स्थिति को बदलने की उम्मीद में जवाबी कार्रवाई करने के लिए दृढ़ है।
शीतकाल सैन्य गतिविधियों के विस्तार के लिए अनुकूल नहीं है, मुख्यतः सामरिक गतिविधियाँ, तोड़फोड़, हवाई हमले, जिनसे सैन्य सफलता मिलने की संभावना कम है। युद्धक्षेत्र की स्थिति स्पष्ट नहीं है, दोनों पक्ष अभी भी दृढ़ता से पीछे न हटने का दृढ़ निश्चय करते हैं और बातचीत का कोई स्पष्ट संकेत नहीं है। लेकिन संघर्ष को हमेशा के लिए नहीं खींचा जा सकता। यदि कोई सैन्य समझौता नहीं होता है, तो अन्य विकल्पों पर विचार करना होगा।
हालाँकि वार्ता के समय और परिणाम की भविष्यवाणी करना मुश्किल है, फिर भी कई परिदृश्य प्रस्तावित किए जा सकते हैं। पहला, रूस को बढ़त तो मिलती है, लेकिन संघर्ष को विजयी रूप से समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं। यूक्रेन को भारी नुकसान होता है, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, आंतरिक और बाहरी दोनों तरफ से भारी दबाव होता है, और उसे युद्धविराम और वार्ता को स्वीकार करना पड़ता है। दूसरा, रूस को नुकसान होता है, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बाहरी दबाव में होता है, युद्धविराम और वार्ता तक पहुँचता है, लेकिन फिर भी "नया क्षेत्र" अपने पास रखता है। तीसरा, युद्ध गतिरोध में है, और रूस और यूक्रेन दोनों एक दीर्घकालिक शांति समझौते पर सहमत होते हैं।
दूसरे परिदृश्य के घटित होने की संभावना कम है; तीसरे परिदृश्य की संभावना और भी कम है। बातचीत की प्रक्रिया कई चरणों से गुज़रनी चाहिए, जिसकी शुरुआत अस्थायी या स्थायी युद्धविराम, यानी विशिष्ट शर्तों के साथ "संघर्ष विराम" से होती है। युद्धविराम, "संघर्ष विराम" को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन किसी भी पक्ष की ओर से इसे तोड़ना आसान है।
मूल समस्या यह है कि यूक्रेन के लिए अपनी ज़मीन छोड़ना स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। जब तक युद्ध के मैदान में अचानक बदलाव न आ जाए, आंतरिक राजनीतिक बदलाव न आ जाए, और पश्चिम हस्तक्षेप करके यूक्रेन को हथियारों और वित्तीय आपूर्ति सीमित न कर दे। पार्टी केंद्रीय समिति के विदेश मामलों के विभाग के पूर्व उप प्रमुख और 13वें चीनी जन राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन की विदेश मामलों की समिति के सदस्य श्री चाऊ ल्यूक के अनुसार, यूक्रेन में संघर्ष को सुलझाने की कुंजी पश्चिमी देशों के हाथों में है। लेकिन अभी तक उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया है। शायद रूस पश्चिम के साथ समझौता स्वीकार कर ले। लेकिन यह भी बहुत मुश्किल है।
यह कहा जा सकता है कि बातचीत का परिदृश्य अभी दूर है और निकट भविष्य में इसके होने की संभावना नहीं है। अगर कोई सफलता नहीं मिलती है, तो सबसे पहला बातचीत का समय 2024 के आखिरी महीनों में हो सकता है, जब युद्ध की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और 60वें अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद।
 |
| 9 दिसंबर को गाजा के राफा में इजरायली हमले के दौरान एक इमारत के ऊपर आग का गोला उठता हुआ। (स्रोत: एएफपी) |
गाजा पट्टी, नाज़ुक उम्मीद
बहुमूल्य और दुर्लभ सात दिवसीय युद्धविराम समाप्त हो गया। इसके तुरंत बाद, अभूतपूर्व भीषण युद्ध छिड़ गया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यह दुनिया का सबसे जटिल, दीर्घकालिक और सबसे कठिन संघर्ष है, जिसके कारण मध्य पूर्व में छह से ज़्यादा युद्ध और कई खूनी झड़पें हुईं।
यह स्थिति तीन मुख्य कारणों से है। पहला, क्षेत्र, जातीयता, संस्कृति और धर्म से जुड़े गहरे, जटिल, अतिव्यापी, लगातार ऐतिहासिक अंतर्विरोध... इसकी प्रकृति दो राज्यों और दो लोगों के बीच सह-अस्तित्व के अधिकार को लेकर एक संघर्ष है, जिसका समाधान बेहद मुश्किल है। दूसरा, इज़राइल और फ़िलिस्तीन के गुटों के बीच आंतरिक अंतर्विरोध, जो सरकार को "सीमा पार करने", समझौता करने और अंतर्विरोध को सुलझाने के लिए एक निर्णायक समाधान खोजने से रोकता है। तीसरा, इस क्षेत्र के देशों और अन्य देशों, खासकर बड़े देशों के रणनीतिक हितों का आकलन। अमेरिका और कुछ देशों ने "पलटवार" कर दिया, तेल अवीव द्वारा पश्चिमी तट पर पुनर्वास क्षेत्रों की स्थापना को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं माना; यरुशलम को इज़राइल की राजधानी के रूप में मान्यता देना, स्थिति को और जटिल बना देता है। अलग-अलग दृष्टिकोण और विरोधी प्रभाव बातचीत के ज़रिए समाधान को और दूर धकेलते हैं।
संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उस हिंसा का विरोध करते हैं जिसके कारण अनेक नागरिक मारे गए हैं और संघर्ष को समाप्त करने का आह्वान करते हैं। इज़राइल व्यापक दायरे, बड़े पैमाने और अधिक तीव्रता के साथ हमले जारी रखे हुए है। इज़राइल इस अवसर का लाभ उठाकर हमास का पूर्ण सफाया करना चाहता है, गाजा पट्टी पर नियंत्रण करना चाहता है और तेल अवीव के विरुद्ध दीर्घकालिक सैन्य कार्रवाई को रोकना चाहता है। हमास सैन्य या राजनीतिक रूप से समाप्त किए जाने को स्वीकार नहीं करता है और दृढ़ता से इसका प्रतिकार करता है। फिलिस्तीन चाहता है कि इज़राइल युद्ध रोक दे, गाजा पट्टी से हट जाए और संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्तावित सीमा को स्वीकार कर ले।
इज़राइल, फ़िलिस्तीन और पूरे क्षेत्र में शांति लाने के लिए दो देशों का सह-अस्तित्व और साथ-साथ रहना ही एकमात्र समाधान है। हालाँकि, इज़राइल और हमास के लक्ष्य और रुख़ एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और अन्य देशों, खासकर बड़े देशों की कार्रवाई, समझौता, दीर्घकालिक युद्धविराम और बातचीत को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त मज़बूत नहीं है। कुछ अन्य देश और इस्लामी संगठन संघर्ष को बढ़ाने वाले कारक हो सकते हैं।
इसलिए, गाजा पट्टी में बातचीत की उम्मीद कमज़ोर बनी हुई है। संघर्ष जटिल और अप्रत्याशित रूप से विकसित हो रहा है। गाजा पट्टी में अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने और आक्रामक अभियान को समाप्त करने के लिए इज़राइल के पास एक से दो महीने का समय है। तेल अवीव अपनी क्षमता के आधार पर ऐसी पूर्व शर्तों के साथ बातचीत के समाधान पर विचार कर सकता है जिन्हें फ़िलिस्तीन स्वीकार नहीं कर पाएगा। सबसे ज़रूरी बात सभी पक्षों, खासकर इज़राइल, के बीच समझौता है।
अगर पक्ष समझौता नहीं करते, तो स्थिति पहले जैसी ही दोहराई जाएगी। लड़ाई कुछ समय के लिए थमेगी, फिर पिछले युद्धों और संघर्षों की तरह फिर से भड़क सकती है। बातचीत तक पहुँचना मुश्किल है, और इसे सभी पक्षों की सहमति से ख़त्म करना और भी मुश्किल है।
[विज्ञापन_2]
स्रोत



![[फोटो] केओ पैगोडा में लगभग 400 साल पुराने खजाने - तुयेत सोन की मूर्ति की पूजा](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F02%2F1764679323086_ndo_br_tempimageomw0hi-4884-jpg.webp&w=3840&q=75)
![[फोटो] लाओस के राष्ट्रीय दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए परेड](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F02%2F1764691918289_ndo_br_0-jpg.webp&w=3840&q=75)







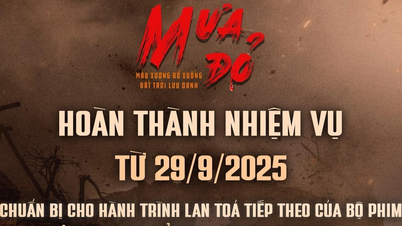



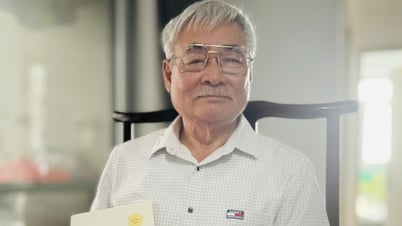








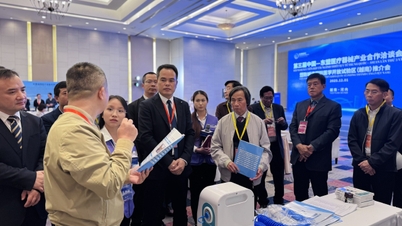















![[वीडियो] चरम जलवायु परिवर्तन से विश्व धरोहर की रक्षा](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/12/03/1764721929017_dung00-57-35-42982still012-jpg.webp)









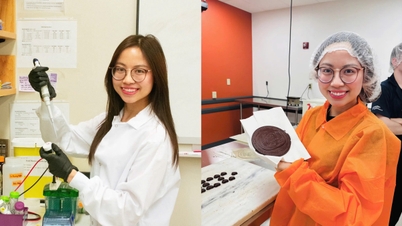






















































टिप्पणी (0)