
5 मार्च की मध्य रात्रि (वियतनाम समय) को, जब फेसबुक एक घंटे के लिए क्रैश हो गया, तो नेटिजन्स अन्य सोशल नेटवर्क पर एक-दूसरे को ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहे थे।
फेसबुक को पिछले मीडिया से अलग करने वाली बात इसकी बढ़ी हुई अन्तरक्रियाशीलता और परम खुलापन है।
मेरी राय में, 5 मार्च की मध्य रात्रि को जब फेसबुक बंद था, तब सोशल नेटवर्क उपयोगकर्ताओं द्वारा एक-दूसरे को खोजने का मूल कारण यह था कि लोगों को हमेशा संपर्क और संचार के किसी न किसी रूप की आवश्यकता होती है।
याद कीजिए, ज़्यादा समय नहीं हुआ, एक दशक से भी ज़्यादा समय पहले, याहू के साथ भी यही हुआ था। जब यह टूल फेल हो गया या काम करना बंद कर दिया, तो लोगों को दूसरे रास्ते ढूँढ़ने पड़े। और फ़ेसबुक बिल्कुल सही समय पर आया।
सोशल मीडिया या इंटरनेट से पहले, लोग भौतिक स्थानों के माध्यम से संवाद करते थे। शायद अब यह भी कुछ अलग है।
बेशक, हम परिवहन के कुछ खास साधनों पर जितना ज़्यादा निर्भर होते हैं, उतनी ही ज़्यादा समस्याएँ पैदा होती हैं। लोग आवागमन और रोज़ी-रोटी कमाने के लिए परिवहन के साधनों का फ़ायदा उठाते हैं, और अब भीड़भाड़ के निश्चित रूप से नकारात्मक प्रभाव होंगे।
यह तो हम जानते हैं, लेकिन भविष्य की तैयारी के लिए हम क्या कर सकते हैं?
निश्चित रूप से, जब सम्पूर्ण जीवन और उपभोग पारिस्थितिकी तंत्र ऑनलाइन डाटाबेस द्वारा संचालित होता है, तो समान कार्यों वाले कुछ अनुप्रयोगों को स्थापित करना आवश्यक होगा।
लेकिन अगला सवाल यह है कि ये एप्लिकेशन कितने समय तक चलते हैं? और क्या हमें इसे दुनिया में कहीं मौजूद सर्वरों पर ही छोड़ देना चाहिए?
इसका जवाब है एक पारंपरिक संचार प्रणाली को फिर से बनाना - वास्तविक जीवन में आमने-सामने का संवाद। मैंने एक टू-डू सूची बनाने की कोशिश की, जिसे दो कॉलम में विभाजित किया गया - ऑनलाइन और ऑफलाइन।
ऑनलाइन श्रेणियाँ त्वरित खोज या सारांश के लिए होती हैं। ऑफ़लाइन कॉलम हमेशा शारीरिक गतिविधियों, खाने-पीने या बस सोने से जुड़ी समान संख्या से भरा होता है।
मैं ऑनलाइन कैसे सो सकता हूँ? लेकिन शायद मैं गलत हूँ, क्योंकि "स्लीप एडिक्ट्स" या "इनसोम्नियाक्स एसोसिएशन" नाम के कई ग्रुप हैं जिनके काफ़ी सदस्य हैं।
मुख्य रूप से, यह अभी भी संचार में विश्वास है।
हम अक्सर कहते हैं कि फेसबुक एक अन्य मानवीय पहचान को व्यक्त करने का स्थान है, और सारा संचार आभासी है।
लेकिन असल में, मानवीय संचार एक ख़ास तरह की सहानुभूति पर आधारित होता है। चाहे हम फ़ेसबुक इस्तेमाल करें या न करें, हम सभी ज़िंदगी में सहानुभूति की तलाश में रहते हैं।
यहीं पर प्रश्न उठता है: क्यों न सहानुभूति की तलाश ऑफलाइन संचार के माध्यम से की जाए?
इसका संबंध हमारे मानसिक जीवन की गुणवत्ता से है। वास्तविक दुनिया में, हमारा मानसिक और बौद्धिक स्थान शायद ऑनलाइन की तुलना में कम जीवंत और समृद्ध है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त जानकारी और डेटा प्रदान करने वाले "ज्ञान के भंडार" का अभाव है।
वह ज्ञान वास्तव में आदान-प्रदान, सीखना और साझा करना है। इसे समाज और समुदाय की एक निरंतरता के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, चाहे मीडिया का क्षेत्र बदलता रहे या मीडिया के कारक ठीक से काम न करें।
[विज्ञापन_2]
स्रोत


![[फोटो] कैट बा - हरा-भरा द्वीप स्वर्ग](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F04%2F1764821844074_ndo_br_1-dcbthienduongxanh638-jpg.webp&w=3840&q=75)





























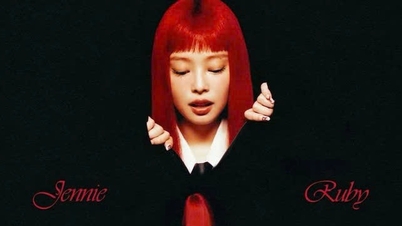















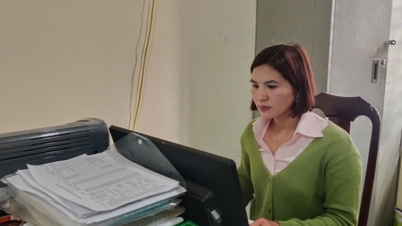








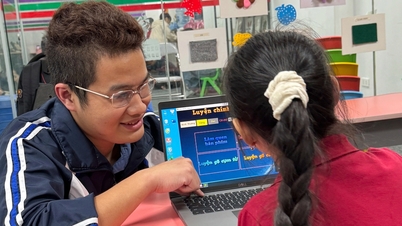


![[VIMC 40 दिन बिजली की गति से] हाई फोंग पोर्ट 2025 तक 2 मिलियन TEUs के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए दृढ़ संकल्पित है](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/12/04/1764816441820_chp_4-12-25.jpeg)























































टिप्पणी (0)