 |
| देशों के लिए डिजिटल वैश्वीकरण (ग्लोबोटिक्स) के लिए तैयार रहना ज़रूरी है। उदाहरणात्मक तस्वीर। (स्रोत: thehansindia) |
1950 के दशक में, विकास सिद्धांत ने आर्थिक विकास के लिए औद्योगीकरण के महत्व पर ज़ोर दिया। चीन उद्योग को अग्रणी बनाने वाले विकास मॉडल का एक विशिष्ट उदाहरण है।
1990 के बाद के आर्थिक विकास मॉडल ने अपतटीयकरण और औद्योगीकरण की लहर शुरू की। उस समय, यह माना जाता था कि विकासशील देशों की समृद्धि वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भागीदारी का परिणाम है। ऐसा करने के लिए, देशों को अपने निवेश वातावरण, नियमों, बुनियादी ढाँचे और व्यापार नीतियों में सुधार करने की आवश्यकता थी।
नया रास्ता?
आज, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर वैश्विक अर्थशास्त्री, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट - आईएमडी (स्विट्जरलैंड) के प्रोफेसर रिचर्ड बाल्डविन ने तर्क दिया है, वैश्वीकरण और डिजिटल (ग्लोबोटिक्स, जिसका मोटे तौर पर अनुवाद डिजिटल वैश्वीकरण के रूप में किया जाता है) का संयोजन वह "द्वार" है जो विकासशील देशों के लिए समृद्धि का एक नया मार्ग खोलता है, जो सेवा मंच पर आधारित वैश्वीकरण का विकास है।
वास्तव में, जहां चीन की आर्थिक सफलता विनिर्माण द्वारा संचालित रही है, वहीं भारत का विकास सेवा क्षेत्र द्वारा संचालित रहा है, जो एक विकासशील देश के लिए अत्यधिक असामान्य विकास मॉडल है।
यह समझना मुश्किल नहीं है कि दुनिया भर की सरकारें विकास के मॉडल के लिए चीन की ओर क्यों देखती रहती हैं। यह मॉडल दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में प्रभावशाली ढंग से फला-फूला है - बड़ी संख्या में किसानों को मज़दूरों में बदल दिया है, मज़दूरी बढ़ाई है, आजीविका में सुधार किया है। करोड़ों लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, एक मज़बूत मध्यम वर्ग का उदय हुआ है, और चीन ने महाशक्ति का दर्जा हासिल किया है।
चीन का रास्ता, जो लंबे समय से अन्य विकासशील देशों के लिए आदर्श रहा है, आसानी से सुलभ नहीं है। चीन में इतने सारे कारक मौजूद हैं कि अन्य अर्थव्यवस्थाओं के लिए उसकी बराबरी करना मुश्किल है।
यहाँ, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा एक बड़ा मुद्दा है और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए वैश्विक दौड़ में भाग लेने की "कुंजी" है। इसलिए, क्षमता के संदर्भ में, आज विकासशील देशों के लिए विनिर्माण क्षेत्र में खुद को "नामांकित" करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूर्वी एशिया, मध्य यूरोप और मेक्सिको के निर्माता औसत से बहुत पीछे हैं।
यहाँ आसान रास्ता, यानी "ऑफशोरिंग", पहले ही चुन लिया गया है। इस बीच, "रीशोरिंग" का चलन अब मुख्यधारा बन रहा है और इसकी विशेषता देशों के भीतर और उनके बीच वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का सरलीकरण है।
वर्तमान वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को नया आकार देने और संचालित करने वाली कुछ विशेषताएं हैं "लचीलापन, अनुकूलनशीलता, डिजिटल प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, पारदर्शी ई-कॉमर्स को बढ़ावा देना; वैश्विक नेटवर्क के भीतर क्षेत्रीय उत्पादन नेटवर्क को बढ़ाना"...
इसलिए, डिजिटल तकनीक विकास का एक और रास्ता खोलती है। वह है दूरस्थ कार्यबल की दूरी को "कम" करना, साथ ही साइबरस्पेस में सहयोग प्लेटफार्मों में निरंतर सुधार करना, सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, दूरसंचार की असाधारण विकास दर के कारण।
इसका प्रमाण अंतर्राष्ट्रीय वस्तु व्यापार में ईबे और अलीबाबा की वृद्धि है।
इस बीच, कम लागत वाला श्रम अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में एक प्रमुख कारक बना हुआ है। महासागर पार स्थित सेवा प्रदाताओं के पास दूर से निगरानी करने, बातचीत करने, कार्य सौंपने, प्रबंधन करने और ऐसे कार्यबल को सुरक्षित रूप से भुगतान करने की क्षमता है, जो मात्र 5 डॉलर प्रति घंटे का भुगतान करता है, जो दुनिया भर के कई देशों में पहले से ही मध्यम वर्ग के जीवन स्तर का मानक है।
इससे व्यवसायों के बीच और यहां तक कि उनके भीतर भी महत्वपूर्ण भिन्नता उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वे विदेशों से सेवाएं खरीदकर/ या आउटसोर्सिंग करके/ या आंतरिक व्यावसायिक प्रक्रियाओं को विदेश में स्थानांतरित करके लागत में कटौती करना चाहते हैं।
भारत इस प्रवृत्ति से लाभान्वित होने वाली एकमात्र अर्थव्यवस्था नहीं है। हालाँकि, भारत की सफलता की कहानी आईटी और लेखा क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर उपलब्ध सेवाओं के कारण उभर कर सामने आती है, जिसके मूलभूत लाभ हैं जैसे कि मज़बूत तकनीकी अवसंरचना, उच्च-स्तरीय उच्च शिक्षा, अच्छी अंग्रेजी भाषा का ज्ञान और बहुत कम संस्थागत बाधाएँ।
नीति का महत्व
पर्यवेक्षकों का कहना है कि एक अग्रणी सेवा निर्यातक के रूप में भारत की तीव्र उन्नति के बारे में दिलचस्प बात यह है कि यह किसी सरकार द्वारा संचालित विकास नीति के कारण नहीं हुई।
यहाँ तक कि भारत के सेवा उद्योग का विकास भी संयोगवश शुरू हुआ। यह भी कहा जाता है कि भारतीय मॉडल को दोहराना मुश्किल है, क्योंकि शुरुआती विकास कुछ हद तक स्वतःस्फूर्त था, इसलिए इसमें काफ़ी समय लगेगा।
2000 के दशक से, भारत विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए आईटी और ज्ञान-आधारित नौकरियों को आउटसोर्स करने के लिए एक प्रमुख स्थान के रूप में उभरा है, और धीरे-धीरे कॉल सेंटरों के साथ-साथ कई अन्य गतिविधियों और प्रक्रियाओं का मेजबान बन गया है, जिनके लिए बहुत अधिक प्रौद्योगिकी श्रम की आवश्यकता होती है।
वास्तव में, प्रारंभ में, सरकारी नीति के कारण नहीं, बल्कि भारत के आर्थिक विकास को “नेतृत्व” देने वाला सेवा क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सीमाओं से “टकराता” रहा, जैसे कि पूंजी तक पहुंच की कमी, कमजोर परिवहन अवसंरचना और अमेरिका, जर्मनी, जापान और चीन जैसे वैश्विक विनिर्माण केंद्रों से बहुत अधिक दूरी...
हालाँकि, फिलीपींस हाल ही में एक सेवा निर्यात केंद्र के रूप में उभरा है। इसने न केवल भारत से सीखा है, बल्कि सेवा क्षेत्र में डिजिटल वैश्वीकरण की लहर पर तेज़ी से सफलतापूर्वक सवार हुआ है, और यह एक सोची-समझी सरकारी रणनीति का परिणाम है।
यह रणनीति मनीला द्वारा कर प्रोत्साहन और विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना के साथ ग्राहक सेवा संस्कृति पर आधारित थी, जिससे सेवा निर्यात व्यवसायों के विकास को प्रोत्साहन मिला।
फिलीपींस चार प्रमुख स्तंभों के आधार पर डेटा सेंटर संचालकों और डेवलपर्स के लिए विशाल संभावनाएं प्रदान करता है: व्यवसायों को क्लाउड कंप्यूटिंग को तेजी से अपनाने में सहायता करना; डिजिटल परिवर्तन के लिए अनुकूल नीतियां स्थापित करना; नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना का निर्माण करना; और एक मजबूत दूरसंचार अवसंरचना का विकास करना।
परिणामस्वरूप, डिजिटल वैश्वीकरण में तेजी लाने की नीति के कारण, 2021 में फिलीपींस की इंटरनेट अर्थव्यवस्था 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ गई और 2025 तक 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।
कुल मिलाकर, विशेषज्ञों का कहना है कि रास्ते साफ करने और चिंताओं का समाधान करने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है, ताकि विश्व अर्थव्यवस्था डिजिटल प्रवाह के विशाल संभावित लाभों से वंचित न रह जाए।
[विज्ञापन_2]
स्रोत


![[फोटो] नेशनल असेंबली के अध्यक्ष ट्रान थान मान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मिले](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/25/1761390815792_ctqh-jpg.webp)



![[फोटो] प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चीन्ह संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मिले](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/25/1761390212729_dsc-1484-jpg.webp)
![[फोटो] प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चीन्ह और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हनोई कन्वेंशन हस्ताक्षर समारोह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/25/1761391413866_conguoctt-jpg.webp)


































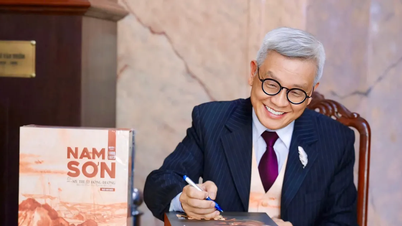










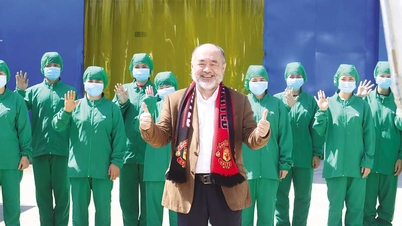

























































टिप्पणी (0)