प्रतिस्पर्धी बिजली बाजार के पक्ष और विपक्ष
ऐसा प्रतीत होता है कि एक विचारधारा यह है कि सभी समस्याओं की जड़ बिजली उद्योग में एकाधिकार है और एकाधिकार को तोड़ने से बिजली उद्योग को विकसित होने में मदद मिलेगी, जैसा कि दूरसंचार और विमानन के साथ हुआ है।
हमें प्रतिस्पर्धी बिजली बाजारों के लाभ और हानि पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है।
दुनिया के हर देश में बिजली पारेषण पर हमेशा से ही स्वाभाविक एकाधिकार रहा है, चाहे वह निजी एकाधिकार हो या राज्य का। अगर एकाधिकार उद्यमों पर छोड़ दिया जाए, तो वे मुनाफ़ा कमाने के लिए कीमतें बढ़ा देंगे और उपभोक्ताओं को नुकसान होगा। यह बाज़ार अर्थव्यवस्था का एक दोष है और इसमें हस्तक्षेप के लिए राज्य के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।
हस्तक्षेप का मूल तरीका यह है कि राज्य बिजली की कीमत तय करे। लेकिन राज्य उस कीमत को तय करने का अपना निर्णय किस आधार पर लेता है?
क्या दुनिया के दूसरे देशों को देखकर घरेलू बिजली की कीमत का हिसाब लगाना संभव है? यह नामुमकिन लगता है क्योंकि हर देश की परिस्थितियाँ बहुत अलग हैं।
सबसे व्यावहारिक मूल्य निर्धारण पद्धति लागत पद्धति है। पिछले वर्ष बिजली उत्पादन और व्यापार की सभी लागतों को जोड़कर, पूरे वर्ष के बिजली उत्पादन से भाग देकर अगले वर्ष की बिजली की कीमत प्राप्त की जाती है। यह वह पद्धति है जिसका उपयोग न केवल वियतनाम, बल्कि कई अन्य देश भी कर रहे हैं।

लेकिन इस दृष्टिकोण के एक अवांछनीय परिणाम हैं। चूँकि बिजली कंपनी जानती है कि इस साल जो खर्च वहन करना है, उसकी भरपाई अगले साल हो जाएगी, इसलिए उसके पास बचत करने का कोई प्रोत्साहन नहीं है। दुनिया के कई देश ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहाँ बिजली कंपनियों के एकाधिकार वाले अपने कर्मचारियों को बहुत ऊँचा वेतन देते हैं और सबसे आधुनिक उपकरण खरीदते हैं।
सरकार ऑडिटर नियुक्त करके लागत की जाँच तो कर सकती है, लेकिन यह तय करना बहुत मुश्किल है कि बिजली उत्पादन और व्यवसाय की लागत वाजिब है या नहीं, और बचत हुई है या नहीं। इसके अलावा, सरकारी अधिकारियों में भी एकाधिकार वाली बिजली कंपनी से बचत करने के लिए कहने की कोई ख़ास प्रेरणा नहीं होती, क्योंकि ऐसा करने से उनके वेतन में कोई वृद्धि नहीं होती?!
बिजली कंपनियों से ऊर्जा दक्षता की माँग करने का प्रोत्साहन केवल उपभोक्ताओं को ही मिलता है। हालाँकि, लाखों उपभोक्ता इतने छोटे और अकुशल हैं कि वे इस लागत-नियंत्रण प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। अगर उपभोक्ता संरक्षण संघ या बिजली का उपयोग करने वाले व्यवसायों के संघ भी होते, तो भी यह अप्रभावी होता।
क्या इस समस्या का कोई समाधान है? खुदरा बिजली बाज़ार में प्रतिस्पर्धा इस विरोधाभास का समाधान हो सकती है।
सबसे पहले, यह कहना ज़रूरी है कि खुदरा बिजली बाज़ार में प्रतिस्पर्धा का मतलब यह नहीं है कि अब एकाधिकार नहीं रहा। ट्रांसमिशन लाइनों पर स्वाभाविक एकाधिकार अभी भी मौजूद है, बस उस एकाधिकार के ग्राहक बदल गए हैं।
प्रतिस्पर्धी मॉडल के तहत, कई मध्यस्थ व्यवसाय होंगे, जो कारखानों के स्रोतों से बिजली खरीदेंगे, एकाधिकार वाली बिजली पारेषण कंपनी से लाइनें किराए पर लेकर बिजली "ले जाएँगे" और ग्राहकों को बेचेंगे। तब उपभोक्ताओं के पास ऐसे कई बिजली खुदरा विक्रेताओं में से चुनने का विकल्प होगा।
इन बिजली खुदरा विक्रेताओं को अभी भी एकाधिकार वाली कंपनियों से लाइनें पट्टे पर लेनी पड़ती हैं। उनके पास उपभोक्ताओं के समान विकल्प नहीं हैं।
लेकिन अब, एकाधिकार के ग्राहक लाखों लोग नहीं, बल्कि कुछ बिजली खुदरा विक्रेता ही हैं। इन व्यवसायों के पास ट्रांसमिशन एकाधिकार से बचत की मांग करने की विशेषज्ञता और प्रेरणा है। सरकार को बस यह सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है कि जो भी बिजली खुदरा विक्रेता ट्रांसमिशन कंपनी से "ज़ोर-ज़ोर से" बचत की मांग करता है, उसके साथ ट्रांसमिशन कंपनी अन्य खुदरा विक्रेताओं की तुलना में भेदभावपूर्ण व्यवहार न करे।
इस प्रकार, खुदरा बिजली बाजार में प्रतिस्पर्धा से पारेषण प्रणाली के निवेश और संचालन में अपव्यय को रोकने में मदद मिलेगी।
प्रतिस्पर्धा की "समस्या"?
हालाँकि, प्रतिस्पर्धा अपनी समस्याओं से रहित नहीं है।
सबसे पहले, प्रतिस्पर्धा से लेन-देन की लागत बढ़ेगी। यह देखा जा सकता है कि बाज़ार में अचानक से ज़्यादा व्यवसाय होंगे, साथ ही मानव संसाधन, बोर्ड, व्यावसायिक संचालन लागत, बातचीत की लागत, विज्ञापन लागत, ग्राहक सेवा लागत आदि भी। ये सभी लागतें कीमत में जुड़ जाएँगी और फिर उपभोक्ताओं को चुकानी होंगी।
क्या यह अतिरिक्त लेन-देन लागत ज़्यादा होगी या अपशिष्ट हानि ज़्यादा होगी? दूसरे शब्दों में, बिजली की अंतिम कीमत बढ़ेगी या घटेगी? इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है क्योंकि यह प्रत्येक देश की परिस्थितियों और नए मॉडल के क्रियान्वयन की गहनता पर निर्भर करता है।
दूसरा, ये खुदरा विक्रेता केवल शहरी क्षेत्रों में ही एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करेंगे, जहाँ बिजली का उत्पादन अधिक है और प्रति यूनिट बिजली की बिक्री पर लाइन किराए पर लेने की लागत कम है। दूरदराज के इलाकों में, जहाँ बिजली का उत्पादन कम है, बिजली आपूर्ति की लागत अधिक है लेकिन राजस्व कम है, ये खुदरा विक्रेता रुचि नहीं लेंगे। उस समय, राज्य को दूरदराज के इलाकों में बिजली की आपूर्ति के लिए, सीधे या एकाधिकार वाली ट्रांसमिशन कंपनी के माध्यम से, हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
यही कारण है कि कई लोग बिजली की खुदरा बिक्री में प्रतिस्पर्धा का विरोध करते हैं, क्योंकि इससे ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि निजी क्षेत्र अच्छे स्थानों पर लाभ कमाने के लिए आगे आ जाएगा, और राज्य अभी भी खराब स्थानों पर कल्याणकारी योजनाओं पर एकाधिकार बनाए रखेगा।
संक्षेप में, प्रतिस्पर्धी खुदरा बाज़ारों का फ़ायदा यह है कि वे एकाधिकारियों के लिए बेहतर लागत नियंत्रण तंत्र बनाते हैं और अपव्यय से बचते हैं। उपभोक्ताओं के पास ज़्यादा विकल्प होते हैं और वे बेहतर बिक्री-पश्चात सेवा का आनंद लेते हैं। हालाँकि, उपभोक्ताओं को फ़ायदा सिर्फ़ शहरी क्षेत्रों में ही मिलता है, और दूरदराज के इलाकों में बदलाव की कोई निश्चितता नहीं है (?)। बिजली की अंतिम कीमत, बढ़ेगी या घटेगी, अभी भी एक प्रश्नचिह्न है।
हालाँकि, एक मूल्य ऐसा भी है जिसे पैसों में नहीं मापा जा सकता, यानी समाज ज़्यादा पारदर्शी होगा। व्यापार और कल्याण के बीच कोई भ्रम नहीं रहेगा, सिर्फ़ तंत्र की बर्बादी से किसी को अचानक फ़ायदा नहीं होगा।
समाज इस सिद्धांत पर चलता है कि न कोई काम करे, न कोई खाए। क्या यह सभ्य है?
गुयेन मिन्ह डुक (सार्वजनिक नीति विशेषज्ञ)
[विज्ञापन_2]
स्रोत





![[फोटो] कैट बा - हरा-भरा द्वीप स्वर्ग](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F04%2F1764821844074_ndo_br_1-dcbthienduongxanh638-jpg.webp&w=3840&q=75)

![[फोटो] वियतनाम फ़ोटोग्राफ़िक कलाकारों के संघ की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F05%2F1764935864512_a1-bnd-0841-9740-jpg.webp&w=3840&q=75)


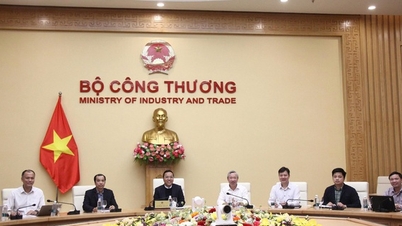

















































































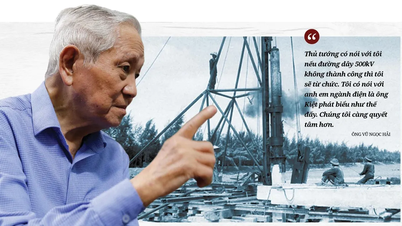




















टिप्पणी (0)