GĐXH - बच्चे भी कमज़ोर होते हैं, खासकर शब्दों के ज़रिए। इसलिए अपने बच्चों को सिखाने के लिए सही शब्द चुनना भी उन्हें बड़ा होने में मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है।
शंघाई (चीन) में लंबे समय से शिक्षिका रहीं सुश्री डुओंग ने बताया: कई वर्षों तक शिक्षिका रहने के बाद, मुझे अक्सर माता-पिता से बच्चों के पालन-पोषण में आने वाली कठिनाइयों के बारे में प्रश्न मिलते हैं: "मेरा बच्चा हमेशा 'मुझे नहीं पता' का जवाब देता है, बात नहीं करना चाहता"; "माता-पिता चाहे कुछ भी कहें, वे सुनते नहीं हैं, लेकिन वे दूसरों की बात सुनते हैं"; "अगर हम बहुत अधिक समझाते हैं, तो बच्चे को गुस्सा आता है, अगर हम कम बोलते हैं, तो हमें डर लगता है कि बच्चा भटक जाएगा, यह वास्तव में कठिन है"...
हालाँकि समस्याएँ कई हैं, लेकिन उन सबका मूल एक ही है: संवाद की समस्या। माता-पिता और बच्चों के बीच संवाद में, भले ही माता-पिता के इरादे अच्छे हों, अक्सर वे वांछित परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते।
कई माता-पिता अक्सर आश्चर्य करते हैं: "हम सही बात क्यों कहते हैं, लेकिन हमारे बच्चे सुनते नहीं?" "यह स्पष्ट रूप से उनके अपने फायदे के लिए है, लेकिन वे इसकी कद्र क्यों नहीं करते?"
वास्तव में, इसका मुख्य कारण यह है कि हम जो सिखाते हैं और जो हमारे बच्चे वास्तव में प्राप्त करते हैं, वह एकसमान नहीं हो सकता।

माता-पिता और रिश्तेदारों के कठोर शब्द और कटु वचन बच्चे के मन में जीवन भर के लिए गहराई से अंकित हो सकते हैं। उदाहरणार्थ चित्र
नीचे कुछ ऐसी बातें दी गई हैं जो माता-पिता अनजाने में अपने बच्चों को चोट पहुंचाते हैं और जिनसे आपको बचना चाहिए:
1. "इसे फिर से करो, बेवकूफ!"
असली विचार: "अगर मैं और मेहनत करूँ, तो मैं सफल हो सकता हूँ।" बच्चा समझता है: "मैं असफल हूँ।"
कुछ असफलताओं का सामना करने पर, बच्चे आसानी से निराश हो जाते हैं। अगर उस समय माता-पिता उन्हें प्रोत्साहित न करें, असफलता की भावनाओं को ठीक से समझाएँ और बाहर न निकालें, तो बच्चा आत्मविश्वास खो सकता है, शर्मीला हो सकता है और दोबारा कोशिश करने से इनकार कर सकता है।
एक कहावत है: "अपने बच्चे की असफलता की आलोचना करने के लिए अपनी भावनाओं का उपयोग न करें।"
जब बच्चे असफल होते हैं, तो माता-पिता को बातचीत में "अंतिम लक्ष्य से शुरुआत करें" सिद्धांत को लागू करना चाहिए: लक्ष्य यह है कि बच्चों को अगली बार असफलता से बचने में मदद की जाए, वर्तमान असफलता से सबक सीखा जाए और बातचीत के लिए भावनाओं का उपयोग करने के बजाय प्रयोग जारी रखने में मदद की जाए।
उदाहरण के लिए, दैनिक जीवन में, अपने बच्चे की छोटी-छोटी गलतियों को नजरअंदाज करने के लिए "चश्मे" के बजाय "आवर्धक कांच" का उपयोग करें और अक्सर प्रशंसा करें: "मैं देख रहा हूं कि आपने सुधार किया है, क्या आप फिर से प्रयास करना चाहते हैं?"।
बच्चे स्वतंत्र व्यक्ति होते हैं जिन्हें सम्मान, समझ और विश्वास की आवश्यकता होती है।
उन्हें आत्म-सम्मान, आत्मविश्वास और स्वतंत्रता विकसित करने के लिए समान संचार और बातचीत की आवश्यकता होती है। भविष्य का सामना करते समय ये सबसे मज़बूत सहारे होते हैं।
2. "तुम्हारी उम्र में, मैं इससे कहीं अधिक कर सकता हूँ"
तुलना करना बच्चों को अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरित करने का अच्छा तरीका नहीं है, कभी-कभी इससे बच्चे स्वयं को हीन और बेकार महसूस करते हैं।
विशेष रूप से, यदि आप एक अभिभावक के रूप में अपने बच्चे की तुलना स्वयं से करते हैं, तो इससे आपके बच्चे को और भी अधिक नुकसान हो सकता है।
वे मनोवैज्ञानिक जटिलताओं से ग्रस्त हो सकते हैं और सोच सकते हैं कि वे अपने माता-पिता के प्यार के लायक नहीं हैं।
यदि तुलना लगातार होती रहेगी तो इससे बच्चों में तनाव पैदा होगा, उनका आत्म-सम्मान कम होगा और यहां तक कि यह उनके अपने माता-पिता से दूर होने का कारण भी बन सकता है।
3. "यह तो एक छोटी सी उपलब्धि है/ इसकी तुलना में क्या है..."
बच्चों को विनम्र होना सिखाना एक आवश्यक गुण है, लेकिन यदि माता-पिता सही तरीके से विनम्र नहीं हैं, तो यह अनजाने में बच्चों के मनोविज्ञान पर एक "कठोर आघात" बन जाएगा।
उदाहरण के लिए, जब कोई बच्चा किसी परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करता है, तो माता-पिता, इस डर से कि उनका बच्चा अहंकारी हो जाएगा, अनजाने में नकारात्मक बातें कह देते हैं: "तुम तो भाग्यशाली हो, यह अन्य बच्चों की तुलना में कुछ भी नहीं है..." या "यह तो एक छोटी सी परीक्षा है, इसमें क्या बड़ी बात है!"
जब बच्चे उच्च अंक प्राप्त करने से खुश और उत्साहित होते हैं, तो उनके माता-पिता के ये नकारात्मक, यहां तक कि "तिरस्कारपूर्ण" शब्द उन पर डाले गए "ठंडे पानी की बाल्टी" के समान होते हैं।
4. "जब तुम ऐसा करते हो तो मुझे दुःख होता है।"
यह कहावत अक्सर माता-पिता द्वारा यह आशा करने के लिए प्रयोग की जाती है कि उनके बच्चे अपना व्यवहार बदल देंगे।
हालाँकि, बच्चों को लग सकता है कि वे अपने माता-पिता के दुःख का कारण हैं, वे दोषी महसूस करेंगे और बहुत दबाव में होंगे।
इससे बच्चे अंतर्मुखी हो सकते हैं, आत्मविश्वास की कमी महसूस कर सकते हैं और गलतियाँ करने से डर सकते हैं। माता-पिता के लिए यह ज़रूरी है कि वे भावनाओं को बच्चों पर हावी न होने दें और सीमाएँ तय करें और उन्हें बनाए रखें।
माता-पिता को यह याद रखना चाहिए कि ये भावनाएं उनकी हैं, उनके बच्चे की नहीं।
5. "यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आप..."
माता-पिता को हमेशा सिरदर्द रहता है क्योंकि उनके बच्चे शरारती और अतिसक्रिय होते हैं। उन्हें अपनी बात मनवाने के लिए, वे अक्सर "धमकी भरे" शब्दों का इस्तेमाल करते हैं।
उदाहरण के लिए, जब बच्चे अवज्ञा करते हैं तो माता-पिता अक्सर ये शब्द कहते हैं: "यदि तुम शांत नहीं बैठोगे, तो तुम्हारा अपहरण कर लिया जाएगा", या "यदि तुम अपने खिलौनों को साफ नहीं करोगे, तो हम उन्हें फेंक देंगे", "यदि तुम मन लगाकर पढ़ाई नहीं करोगे, तो बड़े होने पर तुम्हें कचरा उठाना पड़ेगा",...
माता-पिता अपने बच्चों की परवाह करने वाली चीज़ों को "धमकी भरे" शब्द कहना पसंद करते हैं। वे ये शब्द इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे उनके बच्चे उस "अप्रिय" हरकत को तुरंत बंद कर देते हैं।
हालाँकि, माता-पिता शायद ही कभी जानते हैं कि यह आज्ञाकारिता बच्चे की आत्मा के अंदर के डर से आती है।
"बाहर" तो बच्चे वही करेंगे जो उनके माता-पिता चाहेंगे, लेकिन इसके विपरीत, बच्चे के "अंदर" भी संभावित खतरे मौजूद होते हैं।
जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वे चीजों को समझने लगते हैं और माता-पिता अपने बच्चों को आज्ञाकारी बनाने के लिए हमेशा इस धमकी का उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए धमकियां अधिक से अधिक अप्रभावी होती जाती हैं, यहां तक कि माता-पिता और बच्चों के बीच भयंकर "टकराव" भी हो जाता है।
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रकार के शब्द बच्चों की सुरक्षा की भावना को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं, जिससे धीरे-धीरे उनका अपने माता-पिता पर से विश्वास खत्म हो जाता है।
6. "मुझे तुम पर विश्वास नहीं है"
इस उम्र में अतिसक्रियता के कारण बच्चे कभी-कभी अनावश्यक परेशानी खड़ी कर सकते हैं। अक्सर ऐसी परेशानी का सामना करने पर, माता-पिता अक्सर सवाल पूछते हैं और डाँटते हैं, साथ ही "तुम झूठ बोल रहे हो", "मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है" जैसी बातें भी दोहराते हैं।
ये शब्द एक "चाकू" की तरह होंगे जो माता-पिता और बच्चों के बीच के रिश्ते को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचाएँगे। इससे बच्चे अपने माता-पिता पर भरोसा करना छोड़ सकते हैं और अपने बारे में कुछ भी साझा या बताना नहीं चाहेंगे।
बच्चों को चोट पहुंचाने से बचने के लिए माता-पिता को उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उन पर भरोसा करना चाहिए और बच्चों की हरकतों को समझना चाहिए।

बच्चों को चोट पहुँचाने से बचने के लिए, माता-पिता को उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उन पर भरोसा करना चाहिए और उनकी हरकतों को समझना चाहिए। चित्रांकन
7. "अब आप वयस्क हो गए हैं, आपको अधिक परिपक्वता से सोचना चाहिए।"
जब आप ऐसा कुछ कहते हैं कि "आपको पता होना चाहिए," तो आप अपने बच्चे को दोषी महसूस कराने या बदलने में शर्म महसूस कराने की कोशिश कर रहे होते हैं।
हालाँकि, इससे बच्चे रक्षात्मक हो जाते हैं और सुनने की उनकी संभावना और भी कम हो जाती है। इससे उनका आत्मविश्वास भी कम होता है। दोष देने के बजाय, माता-पिता को अपने बच्चों के साथ मिलकर समस्या का समाधान ढूँढ़ना चाहिए।
ऐसा करके, माता-पिता अपने बच्चों को अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेना और स्वतंत्र सोच कौशल विकसित करना सिखा रहे हैं।
8. "तुम्हें ऐसा होना होगा, वैसा होना होगा..."
प्रसिद्ध स्विस दार्शनिक जीन-जैक्स रूसो ने तीन सबसे "बेकार" पालन-पोषण के तरीके प्रस्तावित किए, जिनमें से उपदेश और नैतिकता कई माता-पिता द्वारा उपयोग किए जाने वाले परिचित तरीके हैं।
जब बच्चे गलती करते हैं, तो माता-पिता को उन्हें पीटना या डांटना सही नहीं है, लेकिन आप माता-पिता को नैतिकता का उपदेश देने के लिए क्यों नहीं प्रोत्साहित करते?
जब आप क्रोधित और परेशान होते हैं, तो क्या आप दूसरे लोगों की "बातें" या "उपदेश" सुनना चाहते हैं? इसका उत्तर है, नहीं।
माता-पिता लंबे समय से "अपने बच्चों के लाभ के लिए" "शिक्षक" की भूमिका निभाने के आदी हो गए हैं, तथा अपने विचारों और धारणाओं को बच्चों पर थोपते रहते हैं।
लेकिन, माता-पिता नहीं जानते कि उनके बच्चे गुस्सा होने पर कैसा महसूस करते हैं और क्या सोचते हैं। ये उपदेश, भले ही बहुत सही लगें, लेकिन उस समय बच्चों को इनकी ज़रूरत नहीं होती। उन्हें असल में सुनने की ज़रूरत होती है।
माता-पिता के रूप में, अपने रूढ़िवादिता और स्वार्थ को एक तरफ रखकर अपने बच्चों से जुड़ें, उनके विचारों को सुनें, उनकी भावनाओं के प्रति सहानुभूति रखें, तथा उनके विचारों और इच्छाओं को बेहतर ढंग से समझें।
एक परिवार का खुश और स्नेही होना या न होना, माता-पिता के व्यवहार और शब्दों पर बहुत हद तक निर्भर करता है। अपने बच्चों को अपनी भावनाओं को स्वाभाविक रूप से विकसित करने दें।
[विज्ञापन_2]
स्रोत: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/giao-vien-lau-nam-nhieu-hoc-sinh-roi-vao-tuyet-vong-vi-thuong-xuyen-phai-nghe-8-cau-noi-nay-cua-cha-me-172250105185457867.htm


![[फोटो] नेशनल असेंबली के अध्यक्ष ट्रान थान मान रूसी संघ की संघीय असेंबली की फेडरेशन काउंसिल के प्रथम उपाध्यक्ष से मिलते हुए](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F02%2F1764648408509_ndo_br_bnd-8452-jpg.webp&w=3840&q=75)





















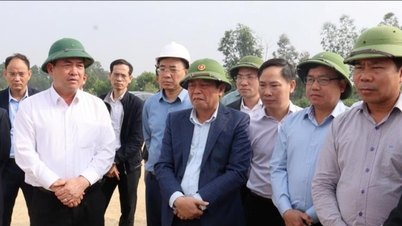



















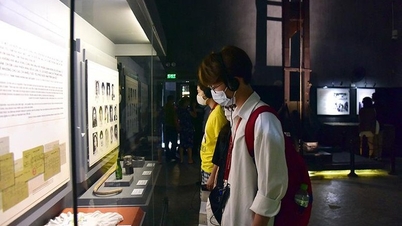

























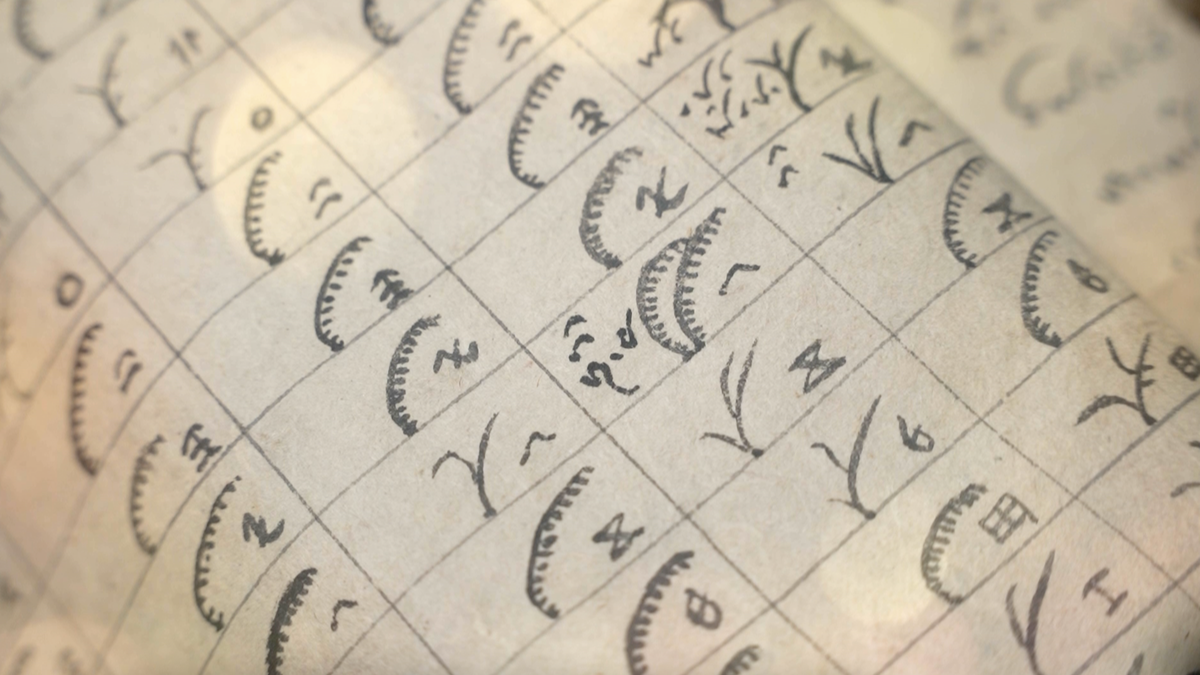



















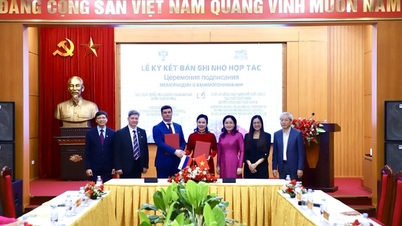























टिप्पणी (0)