कहते हैं कि किसी भी करियर में मिली सफलता बच्चों की शिक्षा में मिली असफलता की भरपाई नहीं कर सकती, इसलिए माता-पिता के लिए बच्चों की शिक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। माता-पिता होने के नाते, हमें खुद से पूछना चाहिए कि हमने अपने बच्चों की शिक्षा में कितने अंक हासिल किए हैं? अगर बच्चों को शिक्षित करना एक होमवर्क है, तो आपको क्या लगता है कि आपके अंक कितने होंगे?
अपने बच्चे की परवरिश करते हुए, क्या आपने उसमें निम्नलिखित में से कोई भी लक्षण देखा है? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि आपकी परवरिश बहुत सफल रही है और आपके बच्चे ने शुरू से ही जीत हासिल की है!

चित्रण फोटो
1. बच्चे ज़िम्मेदारी ले सकते हैं
एक व्यक्ति ने कहा: "मेरी बेटी पड़ोसी के लड़के के साथ बाहर गई, दूसरों को मज़ाक में चिढ़ाती रही और उसका पीछा किया गया। मेरी बेटी जितनी तेज़ी से भाग सकती थी, भागी और घर में सुरक्षित रूप से छिप गई, लेकिन दूसरे लड़के को पकड़ लिया गया और उसे डाँटा गया। मैंने कहानी सुनी और अपनी बेटी से कहा: अब तुम अपने भाई को खेलने के लिए बाहर ले जाती हो, लेकिन अगर तुम किसी दुर्घटना में फंस जाती हो और उसे अकेला छोड़कर भाग जाती हो, तो यह गैर-ज़िम्मेदाराना व्यवहार है। बेटी बहुत देर तक रोती और हिचकिचाती रही, लेकिन आखिरकार दूसरे व्यक्ति से माफी माँगने और अपने भाई को घर ले जाने के लिए बाहर भागी।"
पिता की समय पर शिक्षा ने बच्चों को ज़िम्मेदार बनना सिखाया है। यह एक ऐसा गुण है जो जन्मजात नहीं होता, बल्कि शिक्षा की प्रक्रिया में विकसित होता है। बच्चों में इस गुण को विकसित करने के लिए, माता-पिता को सबसे पहले यह दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि वे उन्हें बिगाड़ेंगे नहीं, बल्कि बच्चों को खुद की देखभाल करना और अपने मामलों की ज़िम्मेदारी लेना सिखाना चाहिए। उदाहरण के लिए, बच्चों को अपना कमरा खुद साफ़ करने दें, अपने गंदे मोज़े खुद धोने दें और अपना होमवर्क पूरा करने दें। अगर बच्चे नियमित रूप से ये काम करें और धीरे-धीरे इनकी आदत डाल लें, तो वे खुद को दूसरों पर निर्भर महसूस नहीं करेंगे और ज़िम्मेदारी का भाव स्वाभाविक रूप से विकसित होगा।
2. बच्चे नियमों का पालन करते हैं
एक बहुत ही "समझदार" माँ, कभी-कभी जहाँ लाइन में लगना ज़रूरी होता था, वह अक्सर अपने बेटे को लाइन में लगने के लिए कहती थी ताकि ज़्यादा देर इंतज़ार न करना पड़े। हालाँकि, बच्चे के किंडरगार्टन में दाखिल होने के बाद, शिक्षक ने सभी बच्चों को चीज़ें लेने के लिए लाइन में लगने को कहा। बच्चा ज़ाहिर तौर पर सबसे पहले नहीं पहुँचा था, लेकिन वह सबसे पहले आना चाहता था, ज़ाहिर है उसे इसकी इजाज़त नहीं थी, इसलिए वह रोने लगा। खिलौनों से खेलते समय, यह बच्चा दूसरे बच्चों के खिलौने भी छीन लेता था, अगर उसे इजाज़त न मिले तो वह तुरंत उन्हें मार देता था। जैसे-जैसे समय बीतता गया, बच्चे के दोस्त उसे "अलग-थलग" कर देते थे, हर कोई उससे दूर रहना चाहता था।
एक कहावत है: जो लोग नियमों की अवहेलना करते हैं, उन्हें अंततः परिणाम भुगतने पड़ते हैं। कुछ बच्चे हमेशा नियमों की अवहेलना करते हैं मानो वे कोई मायने ही नहीं रखते, कूड़ा फेंकते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाते हैं, यहाँ तक कि भीड़-भाड़ वाली जगहों पर शोर मचाते हैं, वगैरह। हालाँकि ये बच्चों की हरकतें हैं, लेकिन ये सीधे तौर पर उनके माता-पिता की उन्हें शिक्षित करने में नाकामी को भी दर्शाती हैं।
किसी भी माता-पिता को अपने बच्चे के विकास में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि कम उम्र से ही कुछ नियम बना दिए जाएँ, ताकि बच्चों को पढ़ाना आसान हो जाए।
3. बच्चे आपके सामने कई अलग-अलग भावनाएँ व्यक्त कर सकते हैं।
आमतौर पर, आप किसी के जितना करीब महसूस करते हैं, उनके सामने अपनी भावनाएँ व्यक्त करना उतना ही आसान होता है। इसी तरह, अगर बच्चे अपने माता-पिता के साथ मनोवैज्ञानिक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं, तो वे कई अलग-अलग भावनाओं, खासकर नकारात्मक भावनाओं, जैसे क्रोध, उदासी आदि को व्यक्त करने का साहस करेंगे।
अगर बच्चा माता-पिता के सामने कम ही भावनाएँ दिखाता है, या सिर्फ़ एक ख़ास तरह की भावनाएँ दिखाता है, तो यह दर्शाता है कि माता-पिता और बच्चों के रिश्ते में कुछ गड़बड़ है। इसलिए, माँओं को अपने बच्चों को उनके गुस्से के लिए दोष नहीं देना चाहिए, और न ही यह सोचना चाहिए कि जो बच्चे बिगड़ैल व्यवहार पसंद करते हैं, वे बिगड़े हुए हैं। इस समय, आपको अपने बच्चे को भावनाओं पर नियंत्रण करना सिखाना होगा ताकि उसके पास बेहतरीन संवाद कौशल हो।
4. जब आप दुविधा में हों तो आपके पास आएं
मनोविज्ञान में एक प्रकार का "सुरक्षित लगाव" होता है, जहाँ लोग किसी भरोसेमंद और आसक्त व्यक्ति से यह सोचकर जुड़े रहते हैं कि वह व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में उनका साथ देगा। ज़ाहिर है, बच्चे के जीवन के शुरुआती दौर में, माता-पिता एक आदर्श व्यक्ति होते हैं।
कई माता-पिता सोचते हैं कि जब बच्चे किसी समस्या का सामना करेंगे और उसे स्वयं हल कर पाएँगे, तो इससे उनकी स्वतंत्रता का विकास होगा। यह सच है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो। दरअसल, बड़े होने की प्रक्रिया में बच्चों के सामने आने वाली कई समस्याएँ उनकी समझ और समाधान की क्षमता से परे होती हैं।
अगर बच्चे की पहली प्रतिक्रिया यह है कि जब ये समस्याएँ आती हैं, तो वह माता-पिता से संपर्क नहीं करता या उन्हें खुद हल करने की कोशिश नहीं करता, तो कभी-कभी यह उसकी आज़ादी में सुधार नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि आप - माता-पिता, अपने बच्चे के साथ संवाद करने में पर्याप्त रूप से सफल नहीं हो पा रहे हैं। जब आपका बच्चा मदद माँगता है, तो आपको अधीर नहीं होना चाहिए या उन्हें दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि समस्याओं को हल करने में उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए।
5. बच्चों पर "लेबल" नहीं लगाया जाता
उदाहरण के लिए, आज बच्चा देर से आया: "तुम इतने आलसी क्यों हो? तुम इतने सुस्त हो कि कुछ भी नहीं कर सकते।" एक और उदाहरण, बच्चा बेसुरी आवाज़ में गाता है: "तुममें वाकई कोई कलात्मक प्रतिभा नहीं है; तुम गाना सीखने के लायक नहीं हो।" या जब बच्चा बोर्डवॉक पर बहुत घबराया हुआ चलता है, तो माता-पिता कहते हैं, "तुम बहुत डरपोक हो।"
माता-पिता अक्सर यह नहीं जानते कि अपने बच्चों को डाँटना, उनकी आलोचना करना, उनकी चिंता करना या उन्हें निराश करना न केवल उन्हें डाँटने या उनकी आलोचना करने पर दुखी करता है, बल्कि और भी ज़्यादा। इन बातों का बच्चों पर एक विचारोत्तेजक प्रभाव पड़ेगा, जिससे वे अनजाने में वैसा ही व्यवहार करने या वैसा बनने लगेंगे। ये बातें बच्चे की आत्मा में बोए गए बीजों की तरह हैं, जो बढ़ते हैं और कभी-कभी बच्चे का असली व्यक्तित्व बन जाते हैं।
कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि अनगिनत बच्चे अपने माता-पिता की गलतफ़हमियों के कारण धीरे-धीरे बुरी आदतें विकसित कर लेते हैं और अंततः वैसे ही इंसान बन जाते हैं जैसा उनके माता-पिता कहते हैं। बचपन में माता-पिता अपने बच्चों को जो लेबल देते हैं, वे जीवन भर उनके साथ रहते हैं। आरोप लगने का आघात अक्सर शारीरिक आघात से कहीं ज़्यादा गंभीर होता है।
6. बच्चों को वह करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो उन्हें पसंद है
जब आपने अपने बच्चे को पियानो सीखने के लिए नामांकित किया, तो क्या आपने उनकी राय पूछी? कुछ माता-पिता अपने बच्चों को रुचि के क्षेत्र विकसित करने की अनुमति नहीं देते हैं, और जिन "शौक" को वे अपने बच्चों को पूरा करने देते हैं, वे वास्तव में ऐसे सपने होते हैं जिन्हें उन्होंने स्वयं पूरा नहीं किया है। कई माता-पिता अनजाने में अपने बच्चों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते हैं, कभी यह नहीं पूछते कि उनके बच्चे क्या करना चाहते हैं।
अगर माता-पिता अपने बच्चों को उनकी प्रतिभा को उजागर करने का मौका नहीं देंगे और उन्हें ऐसे क्षेत्रों में पढ़ने के लिए मजबूर करेंगे जिनमें उनकी रुचि नहीं है, तो बच्चे अपने माता-पिता को निराश करने से डरेंगे और स्वाभाविक रूप से सीखने की प्रक्रिया में बहुत दबाव महसूस करेंगे। नतीजतन, बच्चे को तनावपूर्ण माहौल में रहना पड़ेगा!
माता-पिता का काम अपने बच्चों का मार्गदर्शन करना है, उनके लिए निर्णय लेना नहीं। माता-पिता को अपने बच्चों को स्वतंत्र रूप से यह चुनने देना चाहिए कि वे क्या करना चाहते हैं, और साथ ही धीरे-धीरे उन्हें यह समझने और समझने में मदद करनी चाहिए कि उन्हें वास्तव में क्या पसंद है और उनके भविष्य के लिए क्या ज़रूरी है। सोचिए, क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी आपकी तरह बनें, एक ऐसा काम करें जो उन्हें पसंद न हो, छोड़ना चाहते हों लेकिन हिम्मत न जुटा पाएँ, और अपनी उम्मीदें अगली पीढ़ी पर टिकाएँ? क्या यह एक दुष्चक्र नहीं है?
3 प्रकार के विषाक्त परिवार जो बच्चों को अवसाद का शिकार बनाते हैं
[विज्ञापन_2]
स्रोत



![[फोटो] महासचिव टो लाम रूसी संघ के राष्ट्रपति के अधीन लोक प्रशासन और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अकादमी के निदेशक से मिलते हुए](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F08%2F1765200203892_a1-bnd-0933-4198-jpg.webp&w=3840&q=75)










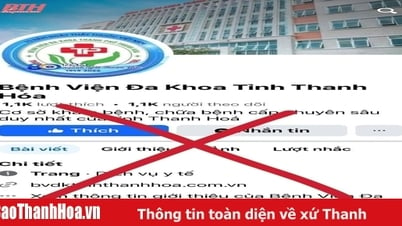




































































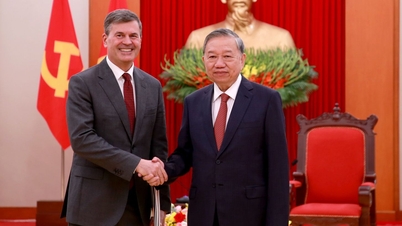












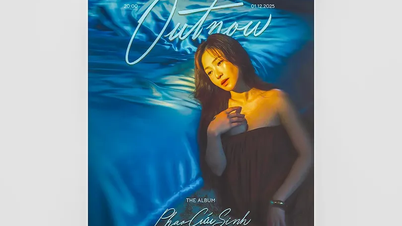
















टिप्पणी (0)